धर्म की व्याख्या
तुम बैठे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ बैठे हो: अपने में ही रमण हो रहा है! तुम अपने में ही डूबे हो, लीन हो, तल्लीन हो। मन कहीं जा ही नहीं रहा है। न भविष्य में जा रहा है, न दूसरे में जा रहा है। क्योंकि दूसरे में भी जाना भविष्य में जाना है। तुम दूसरे का कोई चिंतन ही नहीं कर रहे–सारा चिंतन रुक गया है। तुम विचार ही नहीं कर रहे हो, क्योंकि सभी विचार दूसरे के हैं। तुम सिर्फ हो!
यह स्व-द्रव्य में होना–तुम मात्र हो, कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम कोई संबंध निर्मित नहीं कर रहे। तुम कोई सेतु नहीं बना रहे। दूसरे के पास जाने की कोई आकांक्षा नहीं। दूसरे से दूर जाने की भी कोई आकांक्षा नहीं। दूसरा तुम्हारी कल्पना के लोक में है ही नहीं। बस अकेले तुम अपने से भरे हो! अपने से भरपूर, लबालब, कहीं जाते हुए नहीं! तरंग भी नहीं, लहर भी नहीं। क्योंकि लहर भी कहीं जाती है। तुम बस यहीं हो। ऐसी घड़ी को महावीर कहते हैं धर्म।
लहर उठी–और अगर लहर दूसरे के हित में हुई तो पुण्य, अहित में हुई तो पाप। लहर ही न उठी, तुम स्व-द्रव्य में लीन बैठे रहे–तो धर्म। तो धर्म पुण्य और पाप के पार है।
जो पुण्य और पाप के पार है उसका भविष्य नहीं हो सकता। तुम अपने में तो बस अभी और यहीं हो सकते हो–यही वर्तमान के क्षण में। तुम अपनी आत्म-सत्ता का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि सत्ता उपलब्ध ही है। उसके लिए कल तक रुकने की जरूरत नहीं; यह कहने की जरूरत नहीं कि कल अपने में प्रवेश करूंगा। हां, दूसरे में प्रवेश करना हो तो कल तक रुकना पड़ेगा; दूसरे को राजी करना होगा, समझाना-बुझाना पड़ेगा। लेकिन अपने में प्रवेश करना हो तो इसके लिए तो कल तक छोड़ने की जरूरत नहीं। इसके लिए तो कोई भी साधन जरूरी नहीं है। क्योंकि वहां तो तुम हो ही; सिर्फ थोड़ा विस्मरण हुआ है। स्मरण आते ही तुम अचानक पाते हो कि तुम सदा अपने घर में थे।
यह अपने घर में होना धर्म है।
जिन सूत्र
ओशो

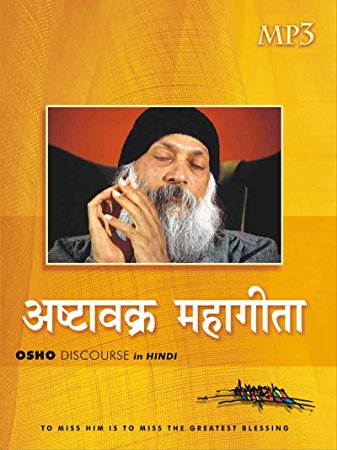

Comments
Post a Comment