तंत्रा-विज्ञान-(Tantra Vision-भाग-01)-प्रवचन-07
तंत्रा-विजन-(सरहा के गीत)-भाग-पहला
सातवां प्रवचन-(सत्य न पवित्र है न अपवित्र)
(दिनांक 27 अप्रैल 1977 ओशो आश्रम पूना।)
सूत्र:
यह है प्रारंभ में, मध्य में, और अंत में
फिर भी अंत व प्रारंभ हैं नहीं और कहीं
जिनके मन भ्रमित हैं, व्याख्यात्मक विचारों से
वह सब हैं दुविधा में, इसीलिए
शून्य और करूणा को वे दो समझते है।
मधु-मक्खियां जानती है, मधु मिलेगा फूलों में
कि नहीं हैं दो, संसार और निर्वाण
भ्रमित लोग समझेंगे पर कैसे यह
भ्रमित कोई जब झांकते हैं किसी दर्पण में
प्रतिविम्ब नहीं, देखते हैं, वे एक चेहरा
वैसे ही जिस मन ने सत्य को नकारा हो
भरोसा वह करता है उस पर जो नहीं है सत्य
यद्यपि छू सकता नहीं कोई सुगंध फूलों की
है यह सर्वव्यापी और एकदम अनुभवगम्य
वैसे ही अनाकृत मन स्वतः
पहचान जाते हैं रहस्यपूर्ण वृतों की गोलाई को
सत्य है। यह बस है। यह मात्र है। यह न कभी अस्तित्व में आता है, न कभी अस्तित्व में आता है और न ही कभी अस्तित्व से जाता है। बस यह यहा है, न कभी आता है न कभी जाता है। यह सदा शेष ही रहता है। सच तो यह है कि जो शेष रहता है उसी को हम सत्य कहते हैं। यह पूर्ण से पूर्ण को निकालने पर पूर्ण ही बचता है। सत्य प्रारंभ में भी है, यह मध्य में भी है, यह अंत में भी है। सच तो यह है कि न कोई प्रारंभ है इसका और न ही कोई अंत। यह संपूर्ण में समाया है, हर एक जगह।
यदि गहरे में देखा जाए तो प्रारंभ भी इसमें है, मध्य भी इसमें है, और अंत भी इसी में है--यह सर्वव्यापी है। क्योंकि केवल यही तो है। यह एक ही सचाई है जो लाखों रूपों में अभिव्यक्त हो रही है। रूप भिन्न हैं, परंतु तत्व, सार वही है।
रूप तो लहरों की भांति हैं और सार समुद्र की भांति है।
स्मरण रखो, तंत्र ईश्वर की बात नहीं करता। ईश्वर की बात करना थोड़ा सा सगुणवादीय है, यह ईश्वर को मनुष्य की प्रतिमा में निर्मित करना है। यह ईश्वर को मानवीय ढंग से सोचना है--यह तो एक सीमा निर्मित करना हुआ। ईश्वर को मनुष्यों की भांति होना चाहिए, यह बात तो सच है--पर उसे घोड़ों की भांति भी तो होना चाहिए, उसे कुत्तों की भांति भी होना चाहिए, उसे चट्टानों की भांति भी तो होना चाहिए, और उसे चांद तारों की भांति भी तो होना चाहिए...उसे तो सबकी ही भांति होना चाहिए। हां, माना एक रूप की भांति मनुष्य को उसमें सम्मिलित किया जा सकता है। परंतु वह एक मात्र रूप हो परमात्मा का हो, बात कुछ जंचती नहीं।
तुम ईश्वर को एक घोड़े की तरह से सोचो--यह कितना अर्थ हीन जान पड़ता है। ईश्वर की कल्पना एक कुत्ते की तरह से करो--कितना अपवित्र सा महसूस होता है। परंतु जरा हमें देखों हम ईश्वर की कल्पना एक मनुष्य के रूप में किए ही चले जाते है--क्यों? इसमें हमें जरा भी अपवित्रता नहीं मालुम होती। परंतु ऐसा कभी सोचा है आपने ये मनुष्य का अहंकार है, आदमी अपने को परमात्म से कम नहीं समझता। वह अपने को ईश्वर का ही छोटा सा रूप मानता है, वह यह मान ही बैठ है कि ईश्वर इसी प्रकार को होगा, उसके भी ऐसी ही नाक होगी, आंखें होगी, इसलिए वह जहां भी ईश्वर की प्रतिमा बनाता है केवल अपने जैसी। बाइबिल में यह कहा गया है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा ही बनाया है, उसने स्वयं की प्रतिमा ही निर्मित की है। निश्चय ही यह बात भी मनुष्य ने ही लिखी होगी। यदि घोड़े अगर अपनी बाइबिल लिखते तो वह यह न लिखते कभी भी। वह तो लिखते कि ईश्वर ने शैतान की प्रतिमा में मनुष्य को बनाया है। क्योंकि ईश्वर-ईश्वर कैसे मनुष्य को अपनी स्वयं की प्रतिमूर्ति में बना सकता है? और मनुष्य घोड़ों के प्रति इतना निर्दयी रहा है, कि घोड़े को तो मनुष्य में ईश्वर जैसी कोई बात नहीं ही जान पड़ती। चाहों तो तुम किसी घोड़े से पूछ सकते हो। हो सकता है, शैतान या हो सकता है बीलजेबब का एक प्रतिनिधि, परंतु ईश्वर तो कदापि ही नहीं।
तंत्र समस्त सगुणवाद को एकदम छोड़ देता है। तंत्र प्रत्येक को अपने सही अनुपात में देखता है, जिसकी जगह जहां है, मनुष्य को उसकी सही जगह पर रखता है। तंत्र एक महान दृष्टि है। यह मनुष्य पर केंद्रित नहीं है। यह किसी पक्षपातपूर्ण भाव पर केंद्रित नहीं है। यह प्रत्येक तथ्य को उसकी सच्चाई की तरह से देखता है, जैसी की वह है, मात्र उसके होने को देखता है। उसके तथाता में, उसकी पूर्णता में, वह कोई ईश्वर की बात नहीं करता। ईश्वर की जगह वह सत्य की बात करता है।
सत्य अ-वैयक्तित है, अव्यक्तिवाचक है। सत्य में सभी के गुण हो सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। बाइबिल कहती है: प्रारंभ में ईश्वर न जगत की सृष्टि की। तंत्र कहता है: कोई प्रारंभ कैसे हो सकता है? और कोई अंत भी कैसे हो सकता है। और जब न कोई प्रारंभ है, और न कोई अंत, तो मध्य भी कैसे होगा। यह तो सब शाश्वतता है, यह समय नहीं है। तंत्र समयातित की एक दृष्टि है। समय में तो एक प्रारंभ भी है, एक मध्य भी है, और एक अंत भी है, परंतु शाश्वता में न तो कोई प्रारंभ है, न मध्य है, और न कोई अंत ही है। यह तो बस है।
सत्य समय का हिस्सा (सामयिक)नहीं है। सच बात तो यह है कि समय सत्य में रहता है। एक लहर की भांति, और आकाश भी सत्य में रहता है एक लहर की ही भांति। इसका विपरीत सच नहीं है। सत्य आकाश में नहीं है, न ही सत्य समय में है। समय और आकाश दोनों ही सम्य में है। वे सत्य के ही प्रकार हैं। जैसे घोड़ा एक रूप है, मनुष्य एक रूप है, वैसे ही आकाश भी एक रूप है, एक बड़ी लहर, वैसे ही समय भी सत्य का एक रूप है।
सत्य तो समयातितता है। सत्य आकाशतितता है। सत्य अतीतता है।
सत्य का अस्तित्व उसके स्वयं में है। बाकी हर चीज का अस्तित्व सत्य के सहयोग से है। सत्य स्वयं-सिद्ध है, बाकी कुछ भी स्वयं-सिद्ध नहीं है। सत्य अस्तित्व का आधार है। अस्तित्व का परम आश्रय है।
तंत्र कोई कर्म कांड निर्मित नहीं करता, कोई पूजा-पाठ निर्मित नहीं करता, कोई मंदिर निर्मित नहीं करता, कोई पुरोहितवाद निर्मित नहीं करता--इस सबकी आवश्यता नहीं है। किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं है। पुरोहित सत्य, और ईश्वर, और स्वर्ग, न जाने हजार चीजों को निर्मित कर लेता है, उनके बारे में बोलता चला जाता है, बिना जरा सा भी जाने कि वे क्यों बोल रहा है। शब्द, कोरे शब्द। उन्होंने कुछ अनुभव नहीं किया है। वे शब्द एकदम रिक्त हैं। एक दम से खाली बिना जानें एक तोता रटन बस और कुछ भी नहीं।
मैं एक बहुत प्रसिद्ध पादरी के विषय में पढ़ रहा था जिसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी।
उसने अपने चिकित्सक को बुलवाया जिसने उसकी अच्छी तरह से जांच की। और कहा: ‘देखो मैं तुमसे स्पष्ट बात कहूंगा, मुझे भय है कि तुम्हारे फेफड़े सही हालत में नहीं है। तुम्हें कुछ महीने स्वीजरलैंड़ में बिताने चाहिए।’
यह कैसे संभव है, डॉक्टर साहब। यह तो असंभव है, मेरे पास इतना धन कहां है? आप तो जानते हैं कि मैं एक गरीब आदमी हूं’, पादरी ने उतर दिया।
यह तो अब तुम्हारे ऊपर है, डॉक्टर ने कहा। या तो स्वीट्जरलैंड या फिर स्वर्ग।’
पादरी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा: ‘ठीक है, तो फिर स्वीट्जरलैंड ही सही।’
स्वर्ग कौन जाना चाहता है? --वह पादरी भी नहीं जो निरंतर उसके विषय में बातचीत करता है। यह एक तरकीब है मृत्यु को सुंदर रंगो में रंगने की, पर पूरे समय तुम जानते तो रहते हो कि यह मृत्यु है। तुम स्वयं को कैसे मूर्ख बना सकते हो?
गुर्जिएफ कहा करता था कि यदि तुम धर्म से छुटकारा पाना चाहते हो, तो किसी पुरोहित के समीप कुछ दिन रहो और तुम धर्म से छुटकारा पा लोगे। शायद साधारण व्यक्ति धोखा खा भी जाए पर पुरोहित कैसे धोखा खा सकता है? वह स्वयं ही तो सारा धोखा निर्मित कर रहा है। कोई पुरोहित कभी धोखा नहीं खाता। वे बात किसी और चीज की करते हैं, वे जानते कुछ और हैं दिखाते कुछ और है। उनकी करनी और कथनी भिन्न होती है।
मैं एक रबाई के बारे में पढ़ रहा था:
एक यहूदी नौजवान अपने रबाई के पास आया। ‘रबाई, क्या एक महत्वपूर्ण मामले पर मैं आपकी सलाह ल सकता हूं?’
‘निश्चित ही,’ उतर मिला।
‘बात कुछ यूं है, मैं दो लड़कियों के प्रेम में हूं...यानि कि मैं सोचता हूं कि मैं उनके प्रेम में हूं। अब एक तो बहुत सुंदर है, परंतु है वह निर्धन, जबकि दूसरी अच्छी तो है पर बहुत सरल है, यद्यपि उसके पास बहुत सा धन है। ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? यदि मेरी जगह आप होते, रबाई, तो आप क्या करते?’
‘देखो,’ रबाई ने कहा, ‘मुझे विश्वास है कि अपने हृदय से तो तुम उस सुंदर स्त्री से ही प्रेम करते हो, इसलिए यदि तुम्हारी जगह मैं होता तो तुरंत जाता और उसी सुंदर स्त्री से विवाह कर लेता।’
‘ठीक है,’ उस नौजवन ने कहा: ‘धन्यवाद, रबाई। मैं यही करूंगा।’
जैसे ही वह लड़का जाने लगा, रबाई ने कहा, ‘सुनो, क्या तुम मुझे उस दूसरी लड़की का पता दे सकते हो?’
तुम्हारे पादरी, रबाई, पुरोहित, मोलवी--वे सब भली-भांति जानते है, कि वे जो भी बातें कर रहे है, वह केवल बाच-चीत है, कोरी बकवास है। यह दूसरों के लिए है--इसका मतलब केवल औरों से है।
तंत्र कोई पुरोहितवाद निर्मित नहीं करता। जब परोहितवाद नहीं होता, तब ही धर्म शुद्ध होता है। पुरोहित को ले आओ और वह इसे विषैला बना कर रख देगा। पुरोहित का काम ही है लोगों को भ्रम जाल में फंसे रखना। इसी में उनका स्वार्थ है, यहीं तो उनके धंधे की कला है।
एक व्यक्ति एक शराबघर में घुसा और अभी उसने पीनी ही शुरू की थी कि उसने एक अन्य शराबी को जो किसी तरह स्वयं को खींच रहा था, लहराते हुए शराबघर से बाहर जाते देखा। और तभी अचानक वह शराबी, जो अभी-अभी बाहर निकला था, इस तरह की मुद्राएं बनाने लगा मानों कि वह कोई कार चला रहा हो। और उसने कार के इंजन और हार्न बजाने की आवाजें भी निकालनी शुरू कर दी।
नवागंतुक तो हैरान रह गया। उसने शराबघर के मालिक से कहा, ‘तुम इस गरीब को बताते क्यों नहीं की वह क्या कर रहा है?’
और शराबघर के मालिक ने कहा, ‘वह हमेशा ऐसे ही करता है। जब भी वह ज्यादा शराब पी लेता है वह यही करता है। अब वह सारी रात ऐसा ही करता रहेगा। वह सारे शहर के चक्कर लगाता रहेगा, वह सोचता है कि वह एक बड़ी कार चला रहा है।’
तब नवागंतुक ने कहा, ‘पर यह बात तुम उसे समझाते क्यों नहीं?’
वाह ये भी खूब रही, ‘भला मैं उसे क्यों समझाऊं? वह अपनी कार की धुलाई के लिए प्रति सप्ताह मुझे एक पौंड जो देता है।’
जब किसी के भ्रम में तुम्हारा विनियोजन होता है, तब उस भ्रम को तुम नष्ट नहीं कर सकते। तुम चाहोगे कि भ्रम बना ही रहे। एक बार जब पुरोहित आ जाता है, तुम्हारे सब भ्रमों में उसका विनियोजन हो जाता है, ईश्वर के विषय में भ्रम, आत्मा के विषय में भ्रम, स्वर्ग के विषय में, नर्क के विषय में भ्रम--अब तुम्हारा बहुत कुछ दाव पर लगा है। अब वह तुम्हारे भ्रमों पर निर्भर है, वह तुम्हारे भ्रमों पर जीता है--वह तुम्हारे भ्रमों का शोषण करता है।
तंत्र एक भ्रम-निवारण है। इसने किसी पुरोहित वाद का सृजन नहीं किया है। तंत्र कहता है कि यह तो तुम्हारे और सत्य के बीच कि बात है। और तुम्हारे और सत्य के बीच में किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं खड़ा होना चाहिए। अपने हृदय को सत्य के प्रति खुला होने दो, सत्य तो अपने में परिपूर्ण है वह माध्यम से विक्रीत हो जाता है। केवल तुम अपने हृदय को सत्य के लिए द्वार भर दे दो। सत्य कि व्याख्या मत करो, न ही इसकी करने की आवश्यकता है। यह क्या है इसे जानने के लिए तुम पर्याप्त हो। सच तो यह है कि जितनी अधिक तुम उसकी व्याख्या करते हो, तुम उससे चुकते ही चले जाते हो। उतना ही उसके जानने की संभावना कम होती चली जाती है। सत्य प्रारंभ में है, मध्य में है, और वह पूर्ण है, हम इतना भी नहीं कह सकते कि वह अंत में है, फिर तो हम सत्य को बांध देते है, यानी सत्य न ही उसका शुरू है और न ही मध्य और न कोई अंत। सत्य गुजर नहीं रहा वह तो स्थिर है।
यही तो पहला सूत्र है सराह का, वह राजा से कहता है:
यह है प्रारंभ में, मध्य में, और अंत में
फिर भी अंत व प्रारंभ हैं नहीं और कहीं
अंत और प्रारंभ कहीं और नहीं हैं। अभी है सत्य-समय, और यहीं है सत्य का आकाश। इसी क्षण, सत्य यहां एकस्थ हो रहा है...अभी। यही क्षण प्रारंभ है, मध्य है, अंत है। अस्तित्व का प्रारंभ कब हुआ यह जानने के लिए तुम्हें अतीत में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्षण तो प्रारंभ है। अस्तित्व का अंत कब होगा यह जानने के लिए तुम्हें भविष्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। हर क्षण हर पल इसका अंत हो रहा है! हर क्षण एक प्रारंभ है, और मध्य है, और अंत है। क्योंकि हर क्षण अस्तित्व नया है कुंवारा है, हर क्षण यह मर रहा है, और प्रत्येक क्षण पैदा भी हो रहा है। हर क्षण सब कुछ अप्रत्यक्षता की स्थिति में चला जाता है, और अगले ही पल वह प्रत्यक्षता की स्थिति में आ जाता है।
अब आधुनिक भौतिक शास्त्र इस बात को स्वीकार कर रहा है कि तंत्र की यह दृष्टि सच हो सकती है। आत्यंतिक रूप से सच हो सकती है। यह हो सकता है हर क्षण प्रत्येक वस्तु अदृश्य हो जाती हो और पुनः वह प्रकट हो जाती हो। इस के बीच का अंतराल इतना छोटा है कि हम इसे देख नहीं पाते। तंत्र कहता है कि यही कारण है कि सत्य हमेशा ताजा, एक दम निरोया अछूता रहता है, अस्तित्व हमेशा ताजा बना रहता है।
मनुष्य को छोड़ कर हर चीज अभी ताजी है, क्योंकि यह मनुष्य ही है जो स्मृति का बोझ, लिए चलता है। इसलिए देखा नहीं मनुष्य कितना अपवित्र, अस्वच्छ, कितना भारी या बोझल होता जा रहा है। वर्ना तो सारा अस्तित्व नया और ताजा है। यह न तो किसी अतीत को ढोता है और न किसी भविष्य की कल्पना ही करता है। यह तो बस यहां है। पूरी तरह से यहां! जब तुम अतीत को ढोते हो तुम्हारे अस्तित्व का एक बड़ा भाग अतीत में संलग्न हो जाता है। उस अतीत से जो अब है ही नहीं। और जब तुम भविष्य की कल्पना करते हो, तुम्हारे अस्तित्व का एक बड़ा भाग भविष्य से संलग्न हो जाता है। उस भविष्य से जो अभी आया ही नहीं है, जो अभी तक है ही नहीं। तुम बहुत ही विरल फैल जाते हो, दोनों आयाम तुम्हें खींच रहे है, तुम्हारा जीवन एक प्रखरता नहीं होता, वह बिखर जाता है, वह तनाव से भर जाता है, उसे साथ लिए चलता है।
तंत्र कहता है कि सत्य को जानने के लिए केवल एक चीज की आवश्यकता होती है: केवल प्रखरता, समग्र प्रखरता की। इस समग्र प्रखरता को कैसे निर्मित किया जाएं? अतीत को त्याग दो और भविष्य को छोड़ दो, तब तुम्हारी सारी जीवन ऊर्जा छोटे से बिंदु पर केंद्रित हो जाती है। और उस केंद्रित होने में तुम एक लपट बन जाते हो, तुम एक जीवंत अग्नि बन जाते हो। तुम वही अग्नि हो जाते हो मूसा ने पर्वत पर जिसे देखा था, और परमात्मा उस अग्नि में खड़ा था। वह अग्नि उसे जला नहीं रही थी। और वह अग्नि उस हरी झाड़ी तक को नहीं जला रही थी, झाड़ी एक दम से प्लवित थी, एक दम जीवंत ताजा लहराती हुई। मानों वह अभी अंकुरित हुई है।
सारा जीवन एक अग्नि है। यह जानने के लिए तुम्हें प्रखरता की जरूरत होती है, वर्ना तो आदमी कुनकुना ही जिए चला जाता है। तंत्र कहता है कि केवल एक ही धर्माज्ञा है: कुनकुने रह कर मत जीयो। यह जीने का ढंग नहीं है, यह तो एक प्रकार कि धीमी आत्म हत्या के जैसा है। जब तुम भोजन कर रहे हो, तुम पूर्णता से उस में डूब जाओ मात्र भोजन ही हो जाओ। तथाकथित संयमी लोगों ने तंत्र की बहुत निंदा की है। वे कहते है: ये तो बस खाओ-पीयो और मोज-मनाओ की सोच वाले लोग है। एक तरह से तो वे जो कहते हैं सच ही है, पर एक और तरह से वह गलत हैं--क्योंकि साधारण खाओ-पीयो, मोज-मस्ती मनाने वाले व्यक्ति में और तंत्र में जीने वाले मनुष्य में जमीन आसमान का अंतर है जो हमें बहार से देखने से महसूस नहीं हो सकते।
तांत्रिक कहता है: यह सत्य को जानने का ढंग है--पर जब तुम भोजन कर रहे हो, तब तुम केवल भोजन ही हो जाओ, उसके रस, गंध, स्वाद में डूब जाओ। न उस समय अतीत को बीच में लाओ न ही भविष्य को। मात्र भोजन हो आप हो, और सब को अदृश्य हो जाने दो। भोजन के प्रति प्रेम, स्नेह, और कृतज्ञता का भाव में डूबे रहो। हर ग्रास को परिपूर्णता चबाओ, उसके रस को अपने पूरे अस्तित्व के साथ घुलन मिलने दो, उसे एक रस होने दो, उसमें कहीं परमात्मा का स्वाद भरा है। अस्तित्व का स्वाद मिलेगा, क्योंकि यह तुम्हें नव जीवन दे रहा है, यह परमात्मा से ही आया है। यह अस्तित्व का ही अंग है। इसी में तुम्हें जीवन देने वाली प्राण ऊर्जा समाहित है। तुम्हारा शरीर इसी प्राण ऊर्जा से चल रहा है, यह शरीर के जीवित रहने में तुम्हारी सहायता करता है। यह मात्र एक भोजन ही नहीं है, भोजन तो एक धारक मात्र है--इसके भीतर जीवन भरा है। यदि तुम मात्र भोजन का स्वाद लेते हो और तुम इसमें अस्तित्व का स्वाद नहीं लेते, तुम एक कुनकुना जीवन ही जी रहे हो। फिर तुम इस बात को भूल ही जाओ कि एक तांत्रिक कैसे जीता है। जब तुम पानी पी रहे होते हो, प्यास ही हो जाओ। इसमें एक प्रखरता होने दो, ताकि ठंडे पानी की प्रत्येक बूंद तुम्हें अत्यंत आनंद प्रदान करे। अपने कंठ में प्रवेश करती पानी की बूंदों से मिलने वाली उस तृप्ति का अनुभव करो, उस जल की एक-एक घूंट में परमात्मा तुम में प्रवेश कर रहा है। तुम्हारी सजगता ही तुम्हें पानी की उन बूंदों में सत्य का ही स्वाद मिलेगा। तुम्हारी तृप्ति तुम्हें आनंद विभोर कर जायेगी।
तंत्र एक साधारण अति-भोग नहीं है, यह असाधारण अति-भोग है। यह साधारण अति-संलग्नता नहीं है, क्योंकि यह स्वयं परमात्मा में अतिसंलग्नता है। परंतु तंत्र कहता है, कि ये जीवन की छोटी-छोटी चीजें ही है जिनसे कि तुम्हें पूर्ण का स्वाद मिलेगा। जीवन कुछ बड़ी चीजें है ही नहीं, हर वस्तु का एक आकार है, वह बहुत ही छोटी है। देखो छोटी सी चीज भी महान हो जाती है, यदि तुम इसमें समग्रता से, पूरी तरह से, परिपूर्णता अपनी सम्पूर्णता से प्रवेश करो।
किसी स्त्री से या पुरूष से संभोग करते समय संभोग ही हो जाओ। सब कुछ भूल जाओ। उस क्षण में वहां कुछ और न होने दो। सारे अस्तित्व को तुम्हारे संभोग में विलीन हो जाने दो। उस संभोग को प्रचंड और निर्दोष होने दो--निर्दोष इस अर्थ में कि उसे भ्रष्ट करने को कोई मन वहां न हो। इसके विषय में चिर मत करो! इसके विषय में कल्पना मत करो! क्योंकि वे सब विचार और कल्पना तुम्हें विरल बनाते हैं, विरल रखते है। सब सोच विचार को अदृश्य रहने दो। कृत्य को पूर्ण होने दो। तुम बस कृत्य में रहो--खोए हुए, संलग्न, मगन--और तब, संभोग से भी तुम परमात्मा को जान लोगे, तुम समाधि को प्राप्त हो जाओगे।
तंत्र कहता है इसे पीने के द्वारा जाना जा सकता है, इसे भोजन के द्वारा जाना जा सकता है, इसे संभोग के द्वारा जाना सकता है। ऐसे ही हजार मार्ग है तुम्हारे दैनिक जीवन में जहां तुम अपने केंद्र तक पहुंच सकते हो। इस हर जगह, हर काने से, हर कोण से जाना जा सकता है--क्योंकि सब कोण उसी के है। यह सब कुछ सत्य ही है जो हमारे चारों और फैला है।
और यह मत सोचना कि तुम भाग्यहीन हो कि प्रारंभ में जब कि परमात्मा ने सृष्टि की रचना की, तब तुम नहीं थे। वह इसे ठीक अभी भी रच रहा है! तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम यहां हो। तुम इसी क्षण सृष्टि रचाते उसे देख सकते हो। और मत सोचना की जब एक धमाके के साथ सृष्टि अदृश्य होगी तब तुम उसे चूक जाओगे--यह इसी क्षण अदृश्य होती है। हर क्षण यह पैदा होती है, हर क्षण यह अदृश्य होती है। हर क्षण यह पैदा होती है, हर क्षण यह मरती है, इसलिए तंत्र कहता है कि तुम अपने जीवन को भी ऐसा ही होने दो--हर क्षण अतीत के प्रति मरना, हर पल पुनः नया निर्मित होना। तुम भार मत ढोओ, खाली रहो।
फिर भी अंत और प्रारंभ हैं नहीं और कहीं वे यहां--अभी है।
जिनके मन भ्रमित हैं, व्याख्यात्मक विचारों से
वह सब हैं दुविधा में, इसीलिए
शून्य और करुणा को वे दो समझते है।
अब सत्य के इस अनुभव को, जो है उसके इस अस्तित्व-गत अनुभव को, तथाता के अनुभव को वर्णन करने के दो ढंग हैं। इसका वर्णन करने के दो तरीके हैं, क्योंकि हमारे पास दो तरह के शब्द हैं: सकारात्मक और नकारात्मक। सराह का जोर नकारात्मक पर है, क्योंकि बुद्ध का जोर उसी पर था।
बुद्ध ने नकारात्मक को बहुत पसंद किया जिसका एक विशेष कारण था। जब तुम अस्तित्व का वर्णन एक सकारात्मक शब्द से करते हो, वह सकारात्मक शब्द इसे एक विशिष्ट सीमा दे देता है। सब सकारात्मक शब्दों की एक सीमा होती है। नकारात्मक शब्दों की सीमाएं नहीं होती, नकार असीम है। उदाहरण के लिए, यदि तुम अस्तित्व को समस्त, ईश्वर, पूर्ण कहते हो, तब तुम इसे एक विशिष्ट सीमा दे रहे हो। जिस क्षण तुम इसे पूर्ण कहते हो, यह भाव उठता है कि बात समाप्त हुई, कि अब यह कोई चलती रहने वाली प्रक्रिया नहीं है। तुम इसे ‘ब्रह्म’ कहा, तब ऐसा लगता है कि जैसे पूर्णता आ गई हो, अब इसमें और अधिक कुछ नहीं है। जब तुम इसे ईश्वर कह देते हो, तुम इसे एक परिभाषा दे देते हो...और अस्तित्व इतना विशाल है, इसे परिभाषित नहीं किया जा सकता, यह इतना विशाल है कि सब सकारात्मक शब्द छोटे पड़ जाते हैं।
इसलिए भगवान बुद्ध ने नकारात्मक को चुना। वह इसे शून्य कहते हैं—ना कुछपन। बस तुम इसका स्वाद लो, इसे इधर-उधर घूमाओ: तुम इसमें कोई सीमा नहीं पा सकते--नाकुछपन। यह असीम है। ईश्वर? तुरंत सीमा आ जाती है। जिस क्षण तुम ‘ईश्वर’ कहते हो, अस्तित्व थोड़ा सा छोटा हो जाता है। जिस क्षण तुम शून्य कहते हो, तमाम सीमाएं अदृश्य हो जाती हैं।
इसी कारण बुद्ध का जोर नकारात्मक पर है, परंतु स्मरण केवल ना कुछ नहीं है। जब बुद्ध नकारत्मकता की बात करते है, उनका तात्पर्य है, ‘शून्य’ यह भी पूर्ण होता है आपने में। कुछ बातें अस्तित्व को परिभाषित नहीं कर सकती क्योंकि सभी कुछ तो इस में समाहित है। यह सम्पूर्ण आयाम के साथ है, सब अंगों को साथ-साथ रख देने पर उनसे भी बड़ा है। अब यह बात-तंत्र की एक दृष्टि ही समझ सकती है। अब इसे थोड़ा समझो...तुम एक गुलाब के फूल को देखते हो। तुम रसायन-शास्त्री के पास जा सकते हो; वह फूल का विश्लेषण कर सकता है, और तुम्हें बता देगा कि किन-किन चीजों के मिलने से फूल बना है, कौन-कौन पदार्थ, किस-किस रसायन, किन्ह-किन्ह रंगो से--यह फूल बना है। वह हर बात का विच्छेदन कर उसे तोड़ कर उस की व्याख्या कर सकता है। परंतु यदि तुम उससे पूछो: ‘इसका सौंदर्य कहां है?’ वह केवल अपने कंधे उचका देगा। वह कहेगा, ‘मुझे तो इसमें कोई सौंदर्य नहीं मिला। मुझे तो इस में केवल यही तत्व मिले है। इतने-रंग, इतने-पदार्थ, इतने रसायन। बस यही सब इसमें था। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ मैंने छोड़ा है, कुछ भी पीछे छूटा नहीं है। आप तौल सकते है, इन सब का कुल इतना ही वजन है, जितना कि इस फूल का। इसलिए कुछ छूटा भी नहीं है।’ तब शायद तुमने धोखा खाया हो, वह सौंदर्य शायद तुम्हारी प्रक्षेपण रहा हो।
तंत्र कहता है कि सौंदर्य है--लेकिन सौंदर्य सभी हिस्सों को साथ रख देने से कहीं अधिक है। समस्त अंगों के योग से अधिक है। यह तंत्र की एक सुंदर दृष्टि है। बहुत ही कीमती, बड़ी महत्वपूर्ण। सौंदर्य उन चीजों से कहीं अधिक है, जिनसे मिलकर यह बनता है।
देखो, एक छोटा बच्चा, प्रसन्नता से खिलखिलाता, किलकारियां मारता, आनंदित, जीवन वहां है, उस छोटे से बच्चे में, अब तुम उसकी चीरफाड़ करो, उसे शल्य-चिकित्सक की मेज़ पर रख दो। तुम वहां क्या पाओगे? न वहां कोई प्रसन्नता होगी, न ही बच्चे कि किलकारियां, न वहां हंसी होगी, और न ही निर्दोषपन पाया जा सकेगा। वहां कोई जीवन ही पाया जा सकेगा। जिस क्षण तुम बच्चे को काटते हो, बच्चा तो जा ही चुका होता है, जीवन तो वहां से अदृश्य ही हो जाता है। परंतु शल्य-चिकित्सक आग्रह करेगा कि कुछ भी नहीं गया है। तुम तौल सकते हो, अंगों का उतना ही वजन है। जितना की समस्त बच्चे का हुआ करता था--कुछ भी छूटा नहीं है, यह एकदम वही बच्चा है। परंतु क्या तुम्हें विश्वास है कि यह वही बच्चा है? और यदि यह बच्चा उस शल्य चिकित्सक का ही होता, तब क्या उसे भी विश्वास होता कि यह वही बच्चा है? मेज़ पर पड़े हुए ये मुर्दा अंग?
कुछ तो ऐसा है जो बच्चे में से अदृश्य हो गया है। हो सकता है कि उस कुछ को तोला न सकता हो? हो सकता है उस अदृश्य को मापा न जा सकता हो? हो सकता है, वह अदृश्य भौतिक न हो, परंतु कुछ तो ऐसा है, जो उसमें से चला गया, निकल गया है। ये बच्चा अब कभी नाच नहीं सकता, किलकारियां नहीं मार सकता, दौड़ नहीं सकता, हंस नहीं सकता, न ही यह कुछ खा सकता है, न ही पियेगा, न रोएगा, न ही सोने के लिए जायेगा, न क्रोधी ही होगा, बस वहीं कुछ था जो उस अदृश्य के चला गया, और मजे कि बात तुम अब इस से प्रेम भी नहीं कर सकते, तुम्हारा प्रेम भी, तुम्हारा लगाव भी उसी अदृश्य से ही था।
तंत्र कहता है कि जोड़ पूर्ण नहीं है। अंगों का कुछ जोड़ पूर्ण नहीं है--पूर्ण तो अंगों के कुल जोड़ से अधिक है। और उस आधिक्य में ही जीवन का अनुभव है।
शून्य होने का अर्थ है, न कुछ हो जाना, सब कुछ को साथ रखने से अस्तित्व नहीं बनता--यह अधिक है। यह अपने अंगों से सदा अधिक है, यह तो इसका सौंदर्य है, यही तो इसका जीवन है। यहीं तो कारण है कि यह इतना आनंदित है। यही तो उत्सव का कारण है।
इसलिए इन दोनों--सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों को हमेशा याद रखो। तंत्र नकारात्मक शब्दों का उपयोग करेगा, विशेषरूप से बौद्ध-तंत्र। और दूसरी और हिंदू-तंत्र सकारात्मक शब्दों का उपयोग करता है, हिंदू-तंत्र और बौद्ध-तंत्र यहीं एक मात्र अंतर है। बुद्ध उस परम को वर्णन करने में सदा ‘न’ का उपयोग करते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि एक बार तुमने उसे गुण प्रदान करना प्रारंभ कर दिया, वे गुण सीमा घटक बन जाते हैं।
इसलिए बुद्ध कहते है: निरस्त करते जाओ--नेति-नेति, कहते जाओ कि यह नहीं है, यह नहीं है, यह नहीं है। और फिर सारे नकारों के बाद भी जो बच जाता है, वही है।
इसलिए याद रखो कि ना कुछ होने का अर्थ खालीपन नहीं है--इसका अर्थ पूर्णता है, परंतु अवर्णनीय पूर्णता। वही अवर्णनियता इस शब्द ना कुछ द्वारा वर्णित की गई है।
जिनके मन भ्रमित हैं, व्याख्यात्मक विचारों से
वह सब हैं दुविधा में,...
सराह कहता है: वे लोग जो बहुत ज्यादा विश्लेषण वादी हैं, व्याख्यावादी हैं, जो मन की श्रेणियों में ही निरंतर विचार करते रहते हैं, वे सदा विभाजित हैं, विभक्त हैं। उनके लिए सदा एक समस्या है। समस्या अस्तित्व में नहीं हैं, समस्या आती है, उनके अपने विभाजित मन से। उनका अपना मन एक अकेली इकाई नहीं है।
अब तुम वैज्ञानिक से भी पूछ सकते हो, वह कहता है मस्तिष्क दो भागों में विभाजित है, बायां और दायां, और दोनों ही अलग-अलग तरह से काम करते है। न केवल अगल-अलग ही बल्कि एक दूसरे विपरीत भी। बाई और का मस्तिष्क विश्लेषणवादी है और दायी तरफ का अंतदृष्टि है। बायीं तरफ का मस्तिष्क गणितशास्त्रीय है, तर्क-शास्त्री है, युक्तिवादी है। दायी तरफ का मस्तिष्क काव्यात्मक, कलात्मक, सौंदर्य-बोधि, रहस्यदर्शी है। और वे दोनों अगल-अलग श्रेणियों में आते है, उन दोनों के बीच एक बहुत छोटा सा सेतु है, बस एक छोटी कड़ी।
कभी-कभी ऐसा हुआ है कि किसी दुर्घटना में वह कड़ी टूट गई और आदमी दो में विभक्त हो गया। द्वितीय विश्वयुद्ध में कई ऐसी घटनाएं हुई जब कि वह कड़ी टूट गई और आदमी दो हो गया, फिर वह एक व्यक्ति न रहा। फिर कभी-कभी वह सुबह को तो एक बात कहता और श्याम होते-होते तक वह भूल जाएगा और कुछ बात कहने लग जायेगा। सुबह को एक गोलार्द्ध काम कर रहा था, श्याम को दूसरा गोलार्द्ध काम करने लगा। और ये बदलते रहते हैं।
आधुनिक विज्ञान को इसमें बहुत गहराई से झांकना होगा। योग ने इसमें बहुत गहराई से छान-बीन की है। योग कहता है: जब तुम्हारी श्वास बदलती है...लगभग चालीस मिनट तक तुम एक नासिका छिद्र से श्वास लेते हो। अभी तक आधुनिक विज्ञान ने इस विषय में विचार नहीं किया है, श्वास क्यों बदलती है? और इसके क्या कारण है? परंतु योग न इस पर गहराई से काम किया है।
जब श्वास तुम्हारी बायीं नासिका से चलती है, तब तुम्हारा दायां मस्तिष्क काम करता है। जब श्वास तुम्हारे दाएं नासिकाछिद्र से चलती है, तब तुम्हारा बायां मस्तिष्क कार्य करने लग जाता है। यह एक प्रकार कि आंतरिक व्यवस्था है ताकि एक मस्तिष्क चालीस मिनट तक कार्य करे। फिर उसे विश्राम मिल जाए। इसलिए बिना ठीक से जाने कि ये क्या है? आदमी ने अनुभव किया है कि चालीस मिनट के बाद तुम्हें अपना कार्य बदल देना चाहिए--यही कारण है कि विद्यालयों, या महाविद्यालयों में चालीस मिनट का एक कक्षा होती है, चालीस मिनट के बाद उसे बदल देते है। मस्तिष्क का एक भाग थक गया, उसे अब विश्राम चाहिए। इसलिए यदि तुम गणित पढ़ रहे हो चालीस मिनट के बाद कविता पढ़ना अच्छा रहेगा। तुम दुबारा गणित पढ़ना शुरू कर सकते हो।
द्वितीय विश्वयुद्ध में यह बात बहुत स्पष्ट हो गई कि यह सेतु बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही कमजोर, किसी भी दुर्घटना से टूट सकता है। और अगर किसी तरह से एक बार यह टूट गया, आदमी फिर दो की भांति काम करने लग जाता है। तब वह एक आदमी नहीं रहता, चालीस मिनट तक वह एक आदमी होता है, दूसरे क्षण वह दूसरा ही आदमी हो जाता है। यदि वह तुमसे धन उधार ले-ले, चालीस मिनट बाद वह इंकार कर देगा, वह कहेगा, ‘तुम क्या बात करते हो मैंने कभी लिया ही नहीं।’ और वह अपनी जगह ठीक ही है, इस बात को स्मरण रखना वह झूठ नहीं बोल रहा है। जिस मस्तिष्क के हिस्से ने धन लिया था, वह तो अब विश्राम कर रहा है, अब वह काम ही नहीं कर रहा है। इसलिए उसे इसकी कोई स्मृति ही नहीं है। जो मस्तिष्क अब कार्य कर रहा है उसने कभी धन उधार लिया ही नहीं। वह अपनी जगह एक दम से सच ही बोल रहा है, सच में ही जिस व्यक्ति ने धन लिया था वो दूसरा ही था, वह एक नहीं तो व्यक्तित्व बन गये है।
और यह उसके साथ भी होता है जिसका की सेतु अभी नहीं टूटा होता है। तुम अपने स्वयं के जीवन को जरा गोर से देखो, और तुम उसमें एक लयबद्धता न पाओगे--निरंतर। अभी एक क्षण पहले तुम अपनी पत्नी के प्रति इतने प्रेमपूर्ण थे, और अचानक कुछ घटता है, और तुम चिंतित होते हो--क्योंकि तुम्हारा सेतु अभी जुड़ा है, तुम्हें थोड़ी सी स्मृति है, थोड़ी देर पहले की घटना अभी आपके श्रवण में बची है। अभी क्षण पहले तुम कितने प्रेम पूर्ण थे, प्रवाहमान थे, और फिर अचानक क्या हुआ? अचानक ही वह प्रवाह टूट गया, तुम जैसे की जम गये। हो सकता है कि तुम अभी अपनी पत्नी का हाथ भी थामे हुए हो, और एक पल में सब बदल गया है। अब मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा सक्रिय हो गया है। अचानक वह भाव वो ऊर्जा पहले वहां पर थी एक पल में गायब हो गई। अब हो सकता है तुम अपनी पत्नी का हाथ छुड़ा कर भाग जाना चाहते हो। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम क्यों इस स्त्री के साथ अपना समय बर्बाद कर रहे हो? इसके पास क्या रखा है? और तुम चिंतित भी होते हो, क्योंकि अभी क्षण भर पहले ही तुम कसम खा रहे थे, ‘मैं तुम्हें सदा प्रेम करूंगा। अभी एक क्षण पहले मैंने कसम खाई थी और अब मैं ये क्या कर रहा हूं अपनी कसम को तोड़ रहा हूं।’
तुम अपने पर क्रोधित भी होते हो, किसी को मार डालना चाहते हो--और कुछ ही मिनट बाद ही क्रोध न जाने कहां चला जाता है। अब तुम क्रोधित नहीं हो। अब तुम उस व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव करने लगते हो, तुम प्रसन्न भी होते हो: ‘अच्छा हुआ कि मैंने उसे मार नहीं डाला।’
अपने मन का अवलोकन करो, और तुम इस बदलाव को निरंतर पाओगे, गेयर लगाता बदलता रहता है।
तंत्र कहता है एकता की एक स्थिति ऐसी भी है, जब कि यह सेतु एक छोटी सी कड़ी बना नहीं रहता बल्कि वास्तव में दोनों मस्तिष्क एक साथ हो जाते हैं। यह एक हो जाना ही सही मायने तुम्हारा मिलन है, अपने अंतस का, अपनी स्त्री पुरुष का अपने द्वैत्व का। क्योंकि इसका एक भाग स्त्रैण है, दूसरा पुरुष का। बायां पुरूष का और दायां स्त्री का। जब तुम किसी स्त्री या पुरुष के साथ संभोग कर रहे होते हो, तब रतिक्षण घटता है, तुम्हारे दोनों मस्तिष्क बहुत ही करीब आ जाते है। तभी तो रतिक्षण घटता है। इसका स्त्री से कुछ लेना-देना नहीं है, इसका बाहर की किसी वस्तु से कुछ लेना-देना नहीं है। यह तो तुम्हारे भीतर ही घट रहा है इसका अवलोकन करो...।
तंत्र ने इस संभोग की घटना का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है, क्योंकि वे सोचते हैं, और वे ठीक हैं, कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी घटना संभोग है, और मनुष्यता का महानतम अनुभव है, रतिक्षण। इसलिए यदि कहीं सत्य तो वह सत्य है, तब किसी अन्य स्थान की अपेक्षा वह सत्य रतिक्षण के क्षण के अधिक समीप होना चाहिए। यह एक साधारण सा तर्क है। इसके लिए बहुत अधिक तार्किक होने की आवश्यता नहीं है। यह तो इतनी स्पष्ट बात है--कि यह आदमी का महानतम आनंद का क्षण है, यह सृष्टि का उत्पत्ति का क्षण है, इस अणु में महान ऊर्जा छिपी है। यह वह पल होना चाहिए, यही वह कुंजी होनी चाहिए, यहीं वह द्वार होना चाहिए, जहां से उस परम में प्रवेश किया जा सके। यही वह क्षण है जो आनंद का द्वार खोल सकता है, भले ही वह लघु है, क्षणांतर में घट जाता है उसे लम्बा किया जा सकता है।
इस लघु क्षण में अनंत का प्रवेश द्वार खुलता है तभी तो इसे प्रकृति ने प्रत्येक जीव में कितना आकर्षण पैदा किया है। उस एक क्षण के लिए न स्त्री रहती है न पुरूष दोनों विलीन हो जाते है। न ही उनका होना होता, तब उस पल अहंकार भी विलीन हो जाता है, उनके खोल अदृश्य हो जाते है।
ठीक-ठीक होता क्या है? तुम शरीर-शास्त्रियों से भी पूछ सकते हो। तंत्र ने बहुत सी बातों का अन्वेषण किया है। थोड़ी सी कुछ बातें: पहली, जब तुम किसी स्त्री से संभोग कर रहे होते हो, और तुम रतिक्षण का आनंद में डूबे हो, इसका उस स्त्री से कोई लेना-देना नहीं है। यह घटना तो तुम्हारे अंदर घट रही होती है, इसका स्त्री के रतिक्षण से कुछ भी लेना-देना नहीं है। उस क्रिया का जरा भी संबंध नहीं है इससे।
जब एक स्त्री को रतिक्षण का अनुभव हो रहा होता है, तब उसे अपने रतिक्षण का अनुभव होता है, इसका तुमसे कुछ लेना-देना नहीं है। हो सकता है तुमने एक प्रारंभ-बिंदु की भांति काम किया हो, परंतु स्त्री का रतिक्षण उसका अपना रतिक्षण है, और तुम्हारा रतिक्षण तुम्हारा अपना है, दोनों का निजी अनुभव है। तुम दानों साथ-साथ जरूर चले थे, सहयोग हो सकता है एक-दूसरे का उस बिंदु तक ले जाने में परंतु अनुभव दोनों का अपना-अपना है। जब तुम्हारा अपना निजी रतिक्षण आता है, तुम आनंद एक दूसरे को बांट नहीं सकते हो। यह तुम्हारा अपना आनंद है। वह यह तो देख सकती है कि कुछ तो घटा है तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारे क्रियाकलापों से परंतु यह तो मात्र एक अवलोकन ही हुआ। वह भी बहार से। वह इसमें साझीदार नहीं हो सकता। जब स्त्री का अपना रतिक्षण होता है, तुम मात्र एक दर्शक ही होते हो, तुम इसमें सहभागी भी नहीं हो सकते।
और यदि तुम दोनों के रतिक्षण साथ-साथ भी घटे, तब भी तुम्हारे रतिक्षण का आनंद अधिक या कम नहीं होगा, यह स्त्री के रतिक्षण से प्रभावित नहीं होगा और न ही स्त्री का रतिक्षण पुरुष के रतिक्षण से प्रभावित होता है। तुम एक दम निजी हो, पूरी तरह से स्वयं में--एक बात। इसका अर्थ है कि सभी रतिक्षण, गहरे में हस्तमैथुन ही है। स्त्री तो बस एक सहायक की भूमिका निभाती है, पुरूष भी एक सहायक ही है, मात्र बहाना है--लेकिन अनिवार्यता नहीं।
दुसरी बात: जिसका की तांत्रिक अवलोकन करते रहे है, वह यह है कि जब रतिक्षण घट रहा होता है, इसका तुम्हारे यौन-केंद्रों से कोई संबंध नहीं होता, कोई भी संबंध नहीं। यदि यौवन केंद्रों का संपर्क तुम्हारे मस्तिष्क से काट दिया जाए, तुम्हें रतिक्षण तो घटेगा ही, पर तुम्हें कोई आनंद प्राप्त नहीं होगा। इसे हम अगर इस तरह से देखे तो कहीं ये हमारे अंदर यौन-केंद्रों पर नहीं घट रहा होता है, जरूर यौन-केंद्र से कोई अंतरिक जुड़ाव मस्तिष्क में घटना प्रारंभ हो जाती है, यह घटना जो काम केंद्र पर हो रही है, यह मस्तिष्क में घट रही है। और आधुनिक खोज इस बात से पूरी तरह से सहमत है।
तुमने प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डेलगाडो का नाम तो सुना होगा। उसने छोटे-छोटे यंत्र बनाए है, वह मस्तिष्क में इलेक्ट्रोड्स लगा देता है और वे इलेक्ट्रोड्स दूर-चलित नियंत्रक से नियंत्रित किये जाते सकते है। तुम अपने पास दूर-चालित नियंत्रकों का एक डिब्बा रख सकते हो। तुम इस यंत्र को अपने खीसे में रख सकते हो जो जब कभी भी तुम रतिक्षण का अनुभव करना चाहो, बस एक बटन दबा दो। इसका तुम्हारे यौन केंद्र से कोई संबंध नहीं है, बटन तो बस तुम्हारे मस्तिष्क में कुछ चीज दबा देगा--सिर के भीतर यह उन केंद्रों को धक्का मार देगा जिन पर धक्का तब लगता है, जब तुम्हारे काम केंद्र से वीर्य स्खलन होता है। काम उर्जा जब केंद्र से मुक्त होती है। परंतु ये यंत्र तुम्हारे मस्तिष्क के उस हिस्से पर सीधा धकेल देगा। और तुम्हें बहुत सुख का अनुभव होगा। तुम्हें लगभग रतिक्षण जैसी अनुभूति प्राप्त होगी। और अगर तुम दूसरा बटन दबा दोगे तो अचानक तुम्हें बहुत क्रोध आ जाएगा। एक और बटन दबा दोगे तुम गहन निराशा में डूब जाओगे। तुम सब तरह के बटन अपने यंत्र में रख सकते हो। और चाहो तो तुम अपने भावदशा को परिवर्तन कर सकते हो।
जब डेलगाडो ने पहली बार अपने जानवरों के साथ प्रयोग किए, खास तौर पर चूहों के साथ, वह हैरान रह गया। उसने अपने सबसे प्यारे चूहे के मस्तिष्क में वे इलेक्ट्रोड लगा दिए--वह चूहा बड़ा प्रशिक्षित था, एक बहुत बुद्धिमान चूहा और डेलगाडो बहुत दिनों से उसके साथ प्रयोग करता आ रहा था। उसने चूहे के सिर में इलैक्ट्रोडस लगा दिए, एक नियंत्रण यंत्र उसके पास रख दिया और उसे प्रशिक्षित भी कर दिया कि इस बटन को दबाना है। जब एक बार उस चूहे को पता चल गया कि ये बटन दबाने से उसे रतिसुख प्राप्त होता है, तब वह तो पागल ही हो गया। एक दिन में उसने उस बटन को करीब छ: हजार बार दबाया, और न व कुछ खाया न कुछ पीया न सोए बस कुछ-कुछ देर बाद वह बटन को दबाता ही रहा जब तक की वह मर न गया। इतने सूख में वह सब भूल गया लगभग वह पागल जैसा हो गया था। मनुष्य के मस्तिष्क के विषय में ये आधुनिक खोज ठीक यही बात कह रही है। जो तंत्र हजारों साल से कहता आया है। एक रतिक्षण के सुख का बाहर से कोई संबंध नहीं है, न बाहर कि किसी स्त्री से, न बाहर के किसी पुरूष से। दूसरी एक बात को भी समझ ले न ही इसका तुम्हारी काम उर्जा से कोई संबंध है। स्त्री तुम्हारी कामऊर्जा को चलायमान कर देती है, ये एक प्राकृतिक की प्रकिृया है, क्रिया तो काम केंद्र पर होती पर सूख जो मिलता है वह मस्तिष्क में घटता है।
यही कारण है कि अश्लील साहित्य का इतना आकर्षण है, क्योंकि अश्लील साहित्य सीधे ही तुम्हारे मस्तिष्क को उत्तेजित करता है, एक सुंदर स्त्री या एक कुरूप स्त्री तुम्हारे रतिक्षण का कोई संबंध नहीं है। एक कुरूप स्त्री से तुम्हें उतना ही रतिसुख प्रदान कर सकती है जितना कि एक सुंदर स्त्री परंतु कुरूप स्त्री को तुम पसंद क्यों नहीं करते? वह तुम्हारे सिर को आकर्षित नहीं करती, बस इतना सी बात है। वर्ना जहां तक रतिसुख का संबंध है, दोनों ही उसमें सक्षम है। कुरूपतम स्त्री हो या सुंदरतम स्त्री हो, या क्ल्योपेट्रा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता--परंतु तुम्हारा सिर तुम्हारा मस्तिष्क आकृति में, सुंदरता में अधिक रुचि लेता है।
तंत्र कहता है कि एक बार हम इस काम-क्षण की सारी कार्यविधि को समझ लें, एक बड़ी समझ का जन्म हो सकता है। एक बात और:
आधुनिक खोज इस बात तक पर राजी है कि संभोग सुख आपके मस्तिष्क में घटता हैं। स्त्री का काम सुख मस्तिष्क के दाएं भाग में घटता है, इस विषय में आधुनिक खोज तो कुछ कहने में सक्षम नहीं है--परंतु तंत्र यह बात कहता है। कि स्त्री का कामसुख उसके दाएं भाग में घटता है। क्योंकि वही स्त्रैण केंद्र है। तंत्र इस विषय में और आगे जाता है, और तंत्र कहता है कि मस्तिष्क के ये दोनों भाग जब समीप आते हैं, यहां आनंद उत्पन्न होता है, संपूर्ण रतिसुख घटता है।
और मस्तिष्क के ये दोनों भाग बड़ी सरलता से समीप आ सकते हैं--जितने कम विश्लेषणवादी तुम होते हो, उतने ही समीप में होते है। इसलिए तो एक व्याख्यात्मक मन कभी आनंदित नहीं हो सकता। आदिवासी लोग अधिक आनंदित होते है, एक गैर-व्याख्यात्मक मन अधिक आनंदित हो सकता है। तथाकथित सभ्य लोगों से, शिक्षित लोगों से, सुसंस्कृत लोगों से। पशु अधिक आनंदित है, पक्षी अधिक आनंदित है, मनुष्यों से। मनुष्य के पास जो व्याख्यात्मक मन है वही इसमें बाधा है, व्याख्यात्मक मन अंतराल को बड़ा कर देता है।
जितना अधिक तर्कपूण ढंग से तुम सोचते हो, दोनों मस्तिष्कों के बीच उतना ही बड़ा अंतराल होता है। जितना कम तर्क पूर्ण ढंग से तुम सोचते हो, उतने ही वे समीप आते हैं। जितनी अधिक काव्यपूर्ण, अधिक सौंदर्यपूर्ण तुम्हारी दृष्टि होगी उतने ही वे अधिक समीप होंगे। जितने वे समीप होते है, उतनी ही प्रसन्नता की आनंद की अधिक संभावना होती चली जाती है।
और अंतिम बात, जिस तक पहुंचने में, मेरे ख्याल में, विज्ञान को कई सदियां लग जाएंगी। अंतिम बात यह है कि आनंद ठीक-ठीक तुम्हारे मस्तिष्क में भी नहीं घटता है--यह तो उस साक्षी में घटता है जो कि मस्तिष्क के दोनों भागों के पीछे खड़ा है। अब अगर यह साक्षी पुरूष मन से अधिक से अधिक आसक्त होता है, तब आनंद उतना अधिक नहीं होगा। अथवा, तुम्हारा साक्षी स्त्री मन से बहुत अधिक आसक्त होता है तब आनंद थोड़ा ज्यादा तो होगा पर बहुत ज्यादा नहीं।
क्या तुम देख नहीं सकते? पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा आनंदित प्राणी है। यही कारण है कि वे अधिक सुंदर, अधिक निर्दोष, दिखाई देती है! वे अधिक समय तक जीती हैं, वे अधिक शांतिपूर्वक, अधिक संतुष्ट जीती है। वे इतनी चिंतित नहीं रहती, वे इतनी अधिक आत्महत्या नहीं करती, वे इतनी अधिक पागल नहीं होती--अनुपात दो गुना है। आदमी दो गुना अधिक आत्महत्या करता है, स्त्रियों की अपेक्षा। और पागल भी करीब-करीब उसी अनुपात में होता है। और तुम्हारे सारे युद्दों को, आतंकवाद को, भी आत्महत्या मान लेते हैं तो आदमी और कुछ करता ही नहीं। सदियों-सदियों से वह युद्ध के नाम पर लोगों को मारता ही तो आ रहा है।
स्त्रैण मन अधिक आनंदपूर्ण है, क्योंकि यह अधिक काव्यात्मक है, अधिक सौंदर्यपूर्ण है, अधिक अंतर्दृष्टि वाला है। परंतु यदि-यदि तुम किसी भी भाग से असकत न होओ, और मात्र साक्षी बने रहो, तब तुम्हारा हर्ष परम पर, अपने उत्कर्ष चरम को छू लेता है। वह एक आत्यंतिक दशा है। इसी हर्ष को हमने आनंद कहां है, इसे जानने के लिए साक्षी को ‘एक’ होना होता है, पूर्णतः एक; तब तुम्हारे भीतर के स्त्री और पुरूष पूरी तरह से अदृश्य हो जाते हैं, आप पूर्ण हो जाते हैं, अद्वत्य-द्वत्वत्व वहां अब खत्म हो गया। एक पूर्णता ही बचती है, केवल होना मात्र, न अब वहां पुरुष है न स्त्री ही, वहां है केवल, ‘साक्षी।’ उस अवस्था में स्त्री और पुरुष दोनों ही मिट जाते है। तब वे एक-दूसरे में खो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, तब रतिसुख का आनंद तुम्हारे क्षण-क्षण का अस्तित्व हो जाता है। और उस अवस्था में काम तो स्वयं अदृश्य हो जाता है--क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं होती। जब कोई व्यक्ति चौबीस घंटे आनंद में ही जीता हो, तब उसकी क्या आवश्यकता रह जाती है।
अपने साक्षीत्व में तुम आनंदपूर्ण हो जाते हो। रतिसुख तब कोई क्षणिक की घटना नहीं रह जाती, तब यह बस तुम्हारा स्वभाव हो जाता है, यही तो समाधि है। हो गया पूर्ण समाधान...तुम पूर्ण हो गए।
जिनके मन भ्रमित हैं, व्याख्यात्मक विचारों से
वह सब हैं दुविधा में, इसीलिए
शून्य और करुणा को वे दो समझते है।....
सराह कहता है कि अस्तित्व शून्यता है, परंतु चिंता मत करो--‘शून्यता’ से हमारा अर्थ यह नहीं है कि यह हर चीज से रिक्त है। सच तो यह है कि यह पूर्ण भरी हुई है--यह इतनी भरी हुई है कि हम इसे न कुछ कहते है। यदि हम इसे कुछ कहें, वह एक सीमा निर्धारित कर देगा, और है यह असीम--इसलिए हम इसे ना कुछ कहते है। परंतु बुद्धों से बार-बार पूछा गया हैं: यदि यह शून्य है तब करुणा कहां से आती है? तब बुद्ध करुणा की बात बार-बार क्यों कहते है?
सराह कहता हैः शून्य और करुणा एक ही ऊर्जा के दो पहलू हैं। अहंकार का अर्थ हैं: मैं कुछ हूं? यदि अस्तित्व शून्य है और मुझे इस अस्तित्व में सहभागी होना है, यदि मुझे इसी अस्तित्व का अंग बनना है, मुझे अहंकार को छोड़ना होगा। ये अहंकार ही मुझे ‘कुछ’ बना रहा है। मुझे एक परिभाषा में बांध रहा है। एक सीमा बना रहा है। जब अस्तित्व बिना किसी स्व के है, यह शून्य है--‘अनंतता’ तब मुझे भी शून्य होना होगा केवल तभी ये दो शून्य एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे में विलीन होने में समर्थ होंगे। मुझे एक निर-अहंकार बनता है, और उस निर-अहंकारिता में ही करुणा है।
अहंकार के साथ लालसा है, निर-अहंकार के साथ करुणा है। अहंकार के साथ हिंसा है, निर-अहंकार के साथ प्रेम है, अहंकार के साथ आक्रामकता है, क्रोध है, क्रूरता है; निर-अहंकार के साथ दया है, करुणा है, समझदारी है, स्नेह है।
इसलिए सरहा कहता है: कि करुणा को आवर्धित नहीं करना है, यदि तुम शून्य में रह सको, करुणा तो स्वतः ही तुम से बहने लगेगी।
मैंने सुना है, एक व्यक्ति अपने बैंक मैनेजर के पास ऋण लेने की प्रार्थना लेकर गया। सब पूछताछ कर लेने के उपरांत बैंक मैनेजर ने कहा: ‘वैसे तो मुझे तुम्हारी प्रार्थना को अस्वीकार कर देने का पूरा अधिकार है, पर मैं तुम्हें एक मजेदार अवसर दूंगा। अब, मेरी दोनों आंखों में से एक आंख शीशे की बनी है। यदि तुम यह बतला दो कि वह आंख कौन सी है, तो मैं आपका ऋण पास कर दूंगा।’
उस व्यक्ति ने गौर से कुछ क्षण तक उस मैनेजर की आंख में देखा, और कहा, ‘यह आपकी दायी आंख है, श्रीमान।’
बैंक मैनेजर ने कहा: ‘बात तो आपने एकदम से सही कही है, परंतु न जाने क्यों मुझे विश्वास नहीं हो रहा, आप मुझे जरा बता पाएंगे कि आपने इसे कैसे पहचाना, कैसे अंदाज लगाया?’
ग्राहक ने कहा: ‘बात यूं है श्रीमान, आपकी दायी आंख में कुछ करुणा जान पड़ती है, इसलिए मैंने सोचा कि इसी को शीशे की होना चाहिए, इधर वाली आंख तो एक दम मृत है पत्थर की तरह उसमें कोई दया का भाव नहीं झलकता।’
अहंकार, हिसाब-किताब लगाने वाला, चालाक मन कभी करुणावान नहीं होता, हो ही नहीं सकता। अहंकार के होने मात्र में ही हिंसा है। यदि तुम हो, तुम हिंसक हो। तुम अहिंसक हो ही नहीं सकते। यदि तुम अहिंसक होना चाहो, तुम्हें अपना ‘मैं’ छोड़ना होगा, तुम्हें एक शून्य होना होगा। उसी शून्य से ही अहिंसा आती है, इसका अभ्यास नहीं करना पड़ता, यह प्रश्न ना कुछ हो जाना है। तब अंतस से करुणा, अहिंसा स्वतः से ही प्रवाहित होती है। यह ‘मैं’ की बाधा है कि तुम्हारी ऊर्जाओं के प्रवाह को रुकावट पहुंचा रही है, वर्ना तो करुणा तो अति सरल है।
सराह कह रहा है: ‘शून्य और करुणा दो नहीं है, तुम शून्य हो जाओ और करुणा वहां होगी। या, तुम करुणा को उपलब्ध हो जाओ, तब तुम पाओगे कि तुम एक शून्य, ना कुछ हो गए हो।’
अस्तित्व का शून्य की भांति यह चरित्र करण अहंकार के संहार की दिशा में एक महान कदम है, और यह संसार को बुद्ध के महानतम योगदानों में से एक है। दूसरे धर्म तो सूक्ष्म ढंगों से उसी अहंकार को आवर्जित किए चले जाते है। सदगुणी व्यक्ति महसूस करने लगता है, ‘मैं तो सदगुणी हूं,’ नैतिक वादी सोचता है, ‘मैं दूसरों से अधिक नैतिक हूं।’ जो भी आदमी का आचरण करता है वह स्वयं को दूसरों से अधिक धर्मात्मा समझता है, पर ये सब तो अहंकार की बातें हैं, और ये मदद नहीं करती हैं। बुद्ध कहते है, अभिवृद्धि प्रश्न नहीं हैं, इस बात की समझ चाहिए कि तुम्हारे भीतर ‘कोई नहीं’ है।
क्या तुमने कभी भीतर झांका है? क्या तुम कभी भीतर गए हो और चारों तरफ देखा है? क्या वहां पर कोई है? तुम किसी को वहां न पाओगे। तुम मौन वहां पाओगे। तुम्हारी वहां किसी से भेंट न हो सकेगी।
सुकरात कहता हैं: स्वयं को जानो। और बुद्ध कहते हैं, यदि तुम जानोगे, तुम पाओगे कि वहां कोई ‘स्वयं’ नहीं है, वहां भीतर कोई नहीं है, वहां शुद्ध मौन है। न तो तुम किसी दीवाल से टकराओगे, न ही तुम किसी व्यक्ति से मिलोगे। यह रिक्तता है। यह इतना शून्य है जितना कि स्वयं अस्तित्व। और उस रिक्तता से ही सब कुछ प्रवाहित हो रहा है, उस शून्य से ही सब कुछ प्रवाहित हो रहा हैं।
मधुमक्खियाँ जानती हैं, मधु मिलेगा फूलों में
कि नहीं हैं दो, संसार और निर्वाण
भ्रमित लोग समझेंगे पर कैसे यह
क्या तुमने कभी गौर किया है? एक सुंदर झील के चारों तरफ बहुत से फूल खिलें हैं। मेंढ़क वहीं उन फूलों की जड़ों के पास ही बैठे हो सकते है। पर उन्हें नहीं पता कि फूलों के भीतर मधु भी होता है।
मधुमक्खियां जानती है,
मधु मिलेगा फूलों में...
जलमुर्गियां, बतख़ें, मछलियां, और मेंढक नहीं जानते यद्यपि वे पौधों के पास ही रह रहे होते हैं। यह जानने के लिए कि फूलों में मधु होता है, मधुमक्खी की तरह है और तपस्वी एक मेढक की तरह है। वह फूलों के बगल में ही रहता है और वह जरा भी सजग नहीं है, इतना ही नहीं कि वह सजग नहीं है, वह इंकार भी करता है। वह सोचता है कि मधुमक्खियां अतिभोगी हैं, कि मधुमक्खियां मूर्ख हैं कि वे स्वयं को नष्ट कर रही हैं।
सराह कहता है कि तपस्वी तो मेढकों जैसे हैं, और मधुमक्खी तांत्रिक जैसी। काम की घटना में ही सर्वोत्कृष्ट भी छिपा है। काम की ऊर्जा में ही वह कुंजी भी है जो कि अस्तित्व के द्वार खोल सकती है। पर मेढक यह बात नहीं जानते। तंत्र कहता है कि यह तो इतना स्पष्ट तथ्य है, कि कामऊर्जा से ही जीवन उत्पन्न होता है--इसका अर्थ है कि काम को जीवन के केंद्र पर होना चाहिए। जीवन काम-ऊर्जा से आता है। एक नया बच्चा काम ऊर्जा के द्वारा पैदा होता है, एक नया प्राणी अस्तित्व में प्रवेश करता है, एक नया अतिथि अस्तित्व में आता है--काम ऊर्जा के द्वारा काम ऊर्जा सर्वाधिक सृजनशील ऊर्जा है। निश्चय ही, यदि हम इसमें गहनता से प्रवेश करे इसे देखें तब हमें इसकी महानता का पता चल सकता है। इसकी अति अधिक सृजनात्मक संभावनाएं ज्ञात हो सकती हैं।
तंत्र कहता है: ‘काम’ तो उस ऊर्जा की सबसे निचली सीढ़ी है, कामवासना की निम्नतम पौडी। यदि तुम इसमें अधिक सजगता से प्रवेश करो और तुम इसमें गहराई से खोज-बीन करो, तुम सर्वोच्च संभावना को, समाधि को, इसमें छिपा हुआ पाओगे।
काम कीचड़ में गिर गई समाधि की तरह है, यह उस हीरे की भांति है जो कीचड़ में गिर गया हो। तुम कीचड़ को साफ कर लो, कीचड़ इसे नष्ट नहीं कर सकता। कीचड़ तो मात्र इसकी सतह तक ही है। तुम बस हीरे को धो दो, और यह पुनः अपनी पूरी कांति से, अपनी पूरी शान से चमकने लग जाता है।
काम में छिपा हुआ है हीरा। प्रेम में छिपा है परमात्मा। जब जीसस कहते हैं कि प्रेम परमात्मा है, उन्हें संभवतः यह विचार तंत्र से ही मिला होगा क्योंकि यहूदियों का परमात्मा तो जरा सा भी प्रेम नहीं है। यह यहूदी परम्परा से तो आ नहीं सकता। यहूदी परमात्मा तो बहुत क्रोधी परमात्मा है।
यहूदी परमात्मा कहता है: ‘मैं बड़ा ईर्ष्यालु हूं, मैं बड़ा क्रोधी हूं। और तुम मेरे विपरीत जाओगे, मैं बदला लूंगा।’ यहूदी परमात्मा तो बड़ा तानाशाह परमात्मा है। प्रेम यहूदी विचार के साथ मेल नहीं खाता। जीसस को यह विचार कहां से मिला कि परमात्मा प्रेम है? इस बात की हर संभावना है कि यह भारत के तांत्रिक के स्कूल से आया है, यहां के तांत्रिकों से ही फैला है।
सराह जीसस से तीन सौ वर्ष पहले हुआ। कौन जानता है? हो सकता है कि ये सराह और उसके विचार ही रहे हों जिन्होंने की यात्रा की हो। ऐसा सोचने के पक्के कारण हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि जीसस भारत आये हों, इस बात की हर संभावना है कि भारत से संदेशवाहिक इसराइल की और गया हों।
परंतु एक बात सुनिश्चित हैं कि यह तंत्र ही है जिसने परमात्मा को प्रेम-ऊर्जा की तरह देखा हैं। परंतु ईसाई चूक गए। जीसस तक ने इशारा किया है, कि ईश्वर प्रेम हैं--वे चूक गए। उन्होंने इसकी व्याख्या ईश्वर-प्रेम की तरह से की--वे चूक गए। जीसस यह नहीं कह रहे हैं कि ईश्वर प्रेमपूर्ण हैं: जीसस कह रहे हैं कि ईश्वर प्रेम है--ईश्वर प्रेम के बराबर है। यह एक सूत्र है: प्रेम बराबर है ईश्वर के। यदि तुम प्रेम में गहरे हो जाओ, तुम ईश्वर को वहां पाओगे, और ईश्वर को पाने का कोई और उपाय नहीं है।
मधुमक्खियां जानती हैं, मधु मिलेगा फूलों में
कि नहीं हैं दो, संसार और निर्वाण
भ्रमित लोग समझेंगे पर कैसे यह...
कौन हैं ये भ्रमित लोग? मेढक, तपस्वी, तथाकथित महात्मागण, जो संसार को इंकार किए जाते हैं, क्योंकि वे कहते हैं कि परमात्मा संसार के विरोध में है। यह मूढ़तापूर्ण है! यदि परमात्मा संसार के विरोध में है तो वह क्यों संसार को रचे चला जाता है? वह बस किसी भी क्षण इसे रोक दे सकता है। यदि वह इसके इतने ही विरोध में है, यदि वह तुम्हारे महात्माओं से सहमत होता तो उसने इसे कभी का रोक दिया होता। परंतु वह तो इसे बनाए ही चला जा रहा है। वह तो इसके विरोध में नहीं जान पड़ता--वह तो पूरी तरह से इसके पक्ष में दिखाई पड़ता है।
तंत्र कहता है परमात्मा संसार के विरोध में नहीं है, संसार और निर्वाण दो नहीं है--वे एक हैं। तपस्वी काम ऊर्जा से लड़ता है, और उस लड़ने के द्वारा ही वह परमात्मा से दूर होता जाता है। जीवन से दूर हट कर जीने लग जाता है। जीवन के ऊर्जावान स्रोत से दूरी बना लेता है। और तब विकृतियां उत्पन्न होती हैं--और वो होंगी ही। जितना अधिक तुम किसी से लड़ते हो, उतना ही अधिक तुम किसी से लड़ते हो, उसके खिलाफ होते जाते हो, उतना ही अधिक विकृत तुम होते चले जाते हो। और फिर तुम तरकीबें ढूंढने लगते हो, पीछे के द्वार से, कि में इस में प्रवेश कर जाऊं, पर वह अति कठिन है।
इसलिए सतह पर तो तपस्वी काम से लड़ता है, जीवन से लड़ता है और भीतर गहरे में वह इसके विषय में कल्पना करने लग जाता है। जितना अधिक वह दमन करता है, उतना अधिक वह इससे ग्रसित होता चला जाता है। तपस्वी एक दमित मानसिकता का व्यक्ति है। तंत्र में जीने वाल एक स्वाभाविक व्यक्ति है। उसके पास कोई भी ग्रस्तताएं नहीं है। परंतु विडंबना देखिए कि तपस्वी सोचना है कि तांत्रिक ग्रसित है, तपस्वी सोचता है कि तांत्रिक तो काम के विषय में बातें करते है, ‘वे काम के विषय में क्यों बातें करते है?’ परंतु असली ग्रस्तता तपस्वी में है, वह इसके विषय में कोई बातचीत नहीं करता। अथवा यदि वह इसके विषय में बातचीत करता भी है, तो वह इसकी निंदा ही करता, इसको गंदा और विकृत भी समझता है। परंतु यह देखने की बात है कि सोचता वह भी रहता है, इसके विषय में चिंतन-मनन करता ही रहता है। उसका मन इसी के आस पास मंडराता रहता है, घूमता रहता है, इसका मंथन करता रहता है।
ईश्वर के विपरीत जाना कठिन है--यदि तुम जाना भी तो इसके विपरीत, तुम्हारी असफलता सुनिश्चित है। मन कोई न कोई तरकीब ढूंढ ही लेता है।
मैंने सुना है, एक यहूदी एक मित्र से बातचीत कर रहा था और उसने कहा, ‘मैं अकेले सोना पसंद करता हूं। मेरा भरोसा ब्रह्मचर्य में है। सच तो यह है कि जब हमारा विवाह हुआ, मैं और मेरी पत्नी अलग-अलग कमरों में रहते आए है।’
‘लेकिन’, मित्र ने कहा, ‘मान लो कि रात में तुम महसूस करो कि तुम थोड़ा सा प्रेम करना चाहोगे, तब तुम क्या करते हो?’
‘ओह,’ यहूदी ने उतर दिया: ‘मैं बस सीटी बजाने लगता हूं।’
मित्र तो और भी अधिक हैरान परेशान हुआ और उसने पूछना जारी रखा, ‘परंतु मान लो बात जरा दूसरे ढंग की हो और तुम्हारी पत्नी महसूस करे कि उसे थोड़े से प्रेम की चाहत है--तब क्या होता है?’
‘ओह’, उसने उतर दिया, ‘वह मेरे दरवाजे तक आती है, उसे खटखटाती है, और पूछती है, ‘ईकी, क्या तुमने सीटी बजाई?’
तुम एक ही कमरे में रहते हो या नहीं इससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है, मन तो कोई न कोई तरकीब खोज ही लेता है। मन सीटी बजाने लग जाता है, और दूसरी और स्त्री तो सीटी बजाना नहीं सीखती, वह इतना बेहूदा होने की जरूरत नहीं लगती। परंतु वह आ तो सकती है। आपके द्वार पर दस्तक दे सकती है। और पूछ सकती है, ‘ईकी, क्या तुमने सीटी बजाई?’
मन अति चालाक है, पर एक बात सुनिश्चित है: तुम जीवन की सच्चाई से भाग नहीं सकते। यदि तुम भागने का प्रयत्न करो भी, तुम्हारा चालाक मन उपाय खोज लेगा और ज्यादा चालाक हो जाएगा। और तुम मन के जाल में और भी अधिक फंस जाओगे। मैं नहीं देख सकता कि कोई तपस्वी कोई सत्य को प्राप्त कर ले--बात असंभव जान पड़ती है। वह तो जीवन को ही इंकार करता है, सत्य को वह कैसे अनुभूत कर सकता है?
सत्य को जीवंत होना ही होगा। सत्य को तो जीवन के साथ खड़े होना होगा, जीवन को पूर्ण स्वीकार करना होगा। इसलिए अपने संन्यासियों से मैं कभी नहीं कहता कि जीवन को छोड़ दो--मैं कहता हूं कि जीवन में रहो। इसमें समग्रता से रहो! वहीं द्वार है, कहीं बाजार में नहीं है, जंगल या हिमालय पर नहीं है।
कि नहीं हैं दो, संसार और निर्वाण
भ्रमित लोग समझेंगे पर कैसे यह...
सराह कहता है, लेकिन मेढक कभी ये बात नहीं समझेंगे? एक मधुमक्खी बन कर! अपने भीतर यह बात एक गहन स्मृति में उतर जाने दो, कम से कम मेरे संन्यासियों के लिए, मधु मक्खी बनो, मेढक मत बनो। जीवन के ये फूल परमात्मा का मधु लिए हुए हैं...इसे इकट्ठा कर लो।
भ्रमित कोई जब झांकते हैं किसी दर्पण में
प्रतिबिंब नहीं, देखते हैं, वे एक चेहरा
वैसे ही जिस मन ने सत्य को नकारा हो
भरोसा वह करता है उस पर जो नहीं है सत्य
मन एक दर्पण की भांति है--यह केवल प्रतिबिंबित करता है, यह तुम्हें मात्र एक छायारूपी अनुभव दे सकता है, वास्तविक कभी नहीं, मौलिक कभी नहीं। यह एक झील की भांति है, और तुम झील में प्रतिबिंबित पूर्णमासी के चांद को देख सकते हो, पर प्रतिबिंबित पूर्णमासी का चांद है, वह कोई वास्तविक चांद नहीं वह तो पड़ रहा उसका बिंब है। वहां तुम वास्तविक चांद को तुम कभी भी न पा सकोगे।
सरहा कहता है:
भ्रमित कोई जब झांकते हैं किसी दर्पण में
प्रतिबिंब नहीं, देखते हैं, वे एक चेहरा...
एक चेहरे को देखने और उसके प्रतिबिंब को देखने में क्या अंतर है? जब तुम दर्पण में चेहरा देखने लग जाते हो, तुम भ्रम में पड़ जाते हो, तुम सोच रहे होते हो, ‘यह मेरा चेहरा है।’ सच पूछो तो यह तुम्हारा चेहरा नहीं है--यह तो मात्र तुम्हारे चेहरे का प्रतिबिंब है, दर्पण में असली चेहरा तो हो ही नहीं सकता। वह तो प्रतिबिंब ही हो सकता है।
मन एक दर्पण है। यह सचाई को प्रतिबिंबित करता है, परंतु यदि तुम उस प्रतिबिंब में भरोसा करना शुरु कर दो, तब तुम असत्य में, छाया में, भरोसा कर रहे होते हो। और वह भरोसा ही एक बाधा बन जाएगा।
सराह कहता है: कि यदि तुम सत्य को जानना चाहते हो, तो मन को उठा कर अलग रख दो--नहीं तो यह प्रतिबिंब बनाता ही चला जाएगा और तुम प्रतिबिंब को ही देखते चले जाओगे। मन को उठा कर अलग रख दो। यदि तुम सच में वास्तविक को जानना चाहते हो, तो प्रतिबिंब के विपरीत हो जाओ।
उदाहरण के लिए, तुम झील में प्रतिबिंबित होते पूरे चांद को देखते हो। अब, पूरे चांद को खोजने तुम कहां जाओगे? क्या तुम झील में छलांग लगा दोगे? क्या तुम चांद को पाने के लिए झील में गहरा गोता लगाओगे? तब तो तुम इसे कभी भी नहीं पा सकोगे। तुम स्वयं को भी खो दे सकते हो। यदि तुम सच में ही असली चांद को देखना चाहते हो, फिर प्रतिबिंब के विपरीत जाओ। उसके ठीक उलटी दशा में, तब तुम एक न एक दिन चांद को पा लोगे। मन में मत जाओ, मन से ठीक विपरीत दिशा में जाओ।
तुम्हारा मन विश्लेषण करता है, तुम संश्लेषण करो। मन के तर्क में विश्वास करता है, तुम तर्क में विश्वास मत करो, मन बहुत हिसाबी-किताबी है, मन बहुत चालाक है, तुम सरल हो जाओ। विपरीत दिशा में चलो! मन सबूत मांगता है, पूछता है, तर्क करता है। श्रद्धा का यही तो अर्थ है, विपरीत दिशा में जाओ। मन बड़ा संदेहवादी है। यदि तुम संदेह करते हो, तुम मन में जाते हो। यदि तुम संदेह नहीं करते, तुम मन के विपरीत जाते हो। संदेह मत करो! जीवन जीने के लिए है, संदेह करने के लिए नहीं। जीवन पर तो भरोसा रखना है। भरोसे के हाथ में हाथ डाल कर चलो और तुम सत्य को पा लोगे; संदेह के साथ रहो और तुम पागल हो जाओगे।
सत्य की खोज मन से ठीक विपरीत दिशा में खोज है, क्योंकि मन एक दर्पण है। यह प्रतिबिंब बनाता है। मन को उठा कर एक और रख देना ही तो ध्यान है।
जब तुम सचाई को बिना विचारों द्वारा इसे प्रतिबिंबित किए, सीधे ही देख पाते हो, सत्य यहां अभी यहां होता है। तब तुम सत्य होते हो और सब-कुछ सत्य होता है। मन तो भ्रम की, छलावे की, स्वप्न की एक बड़ी कार्यकारी क्षमता है।
यद्यपि छू सकता नहीं कोई सुगंध फूलों की
है यह सर्वव्यापी और एकदम अनुभवगम्य
वैसे ही अनाकृत मन स्वतः
पहचान जाते हैं रहस्यपूर्ण वृतों की गोलाई को
यह एक महान सूत्र है:
यद्यपि छू सकता नहीं कोई सुगंध फूलों की
है यह सर्वव्यापी और एकदम अनुभवगम्य
वैसे ही अनाकृत मन स्वतः
पहचान जाते हैं रहस्यपूर्ण वृतों की गोलाई को...
परंतु केवल तुम इसे सूंघ सकते हो, यह तुम्हें चारों और हो सकती हैं, पर तुम्हारे नासापुट ही इसे महसूस कर सकते है। यह तुम्हें चारों तरफ से घेर लेती है। तुम इसे छू नहीं सकते हो, यह मूर्त नहीं है, यह स्पर्शनीय नहीं है, परंतु तुम इसकी सहर्स्पशता को महसूस कर सकते हो। परंतु अगर तुम मूर्तता को ही सत्य की कसौटी बना लोगे, तब तो तुम यही कहोगे कि यह सत्य नहीं है, सत्य विचाराधीन नहीं है। यदि तुम विचार करोगे, तुम इससे चूक जाओगे।
सत्य का अनुभव तो किया जा सकता है, पर इसे छुआ नहीं जा सकता। सत्य को अनुभूत तो किया जा सकता है, पर इसे निष्कर्षित नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक फूल की सुगंध को आंखों से देखा नहीं जा सकता, कानों से सुना नहीं जा सकता...परंतु अगर तुम यही मापदंड बना लो कि, ‘जब तक कि मैं सुगंध को सुन न लूं, मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगा।’ तब तो तुम बाधाएं निर्मित कर रहे हो, और तब तुम इसे कभी नहीं जान पाओगे।
और धीरे-धीरे, तुम इस पर भरोसा न करो, यदि तुम भरोसा ही न करो, तुम इसे सूंघ पाने की क्षमता ही खो दोगे--क्योंकि जिस क्षमता का भी उपयोग नहीं किया जाता, जिस पर भरोसा नहीं किया जाता, वह अनुपयोगी हो जाती है, वह धीरे-धीरे अक्षम हो जाती है, भरोसा भी एक प्रकार कि क्षमता ही है, तुम संदेह के साथ इतने लंबे समय तक रहे हो, इतने लंबे समय से तुम संदेह के साथ गठजोड़ किए चले आ रहे हो, तुम कहते हो कि ‘मुझे पहले विचारपूर्ण सबूत चाहिए--मुझे संदेह है।’ इसलिए तुम संदेह के साथ रहे जाते हो और सत्य केवल भरोसे से ही जाना जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि सुगंध केवल सुंघने से ही जानी जा सकती है। यह है, यदि तुम सुंध सको, सत्य है यदि तुम भरोसा कर सको।
श्रद्धा, भरोसा, निष्ठा--बस एक बात की और इंगित करते है, कि सत्य को जानने की क्षमता संदेह नहीं है। संशयालुता नहीं है। यदि तुम संदेह पर जोर दोगे, तुम संदेह में ही रहोगे।
है यह सर्वव्यापी और एकदम अनुभवगम्य...
श्रद्धा के साथ, यह तुरंत है! एक क्षण भी नहीं खोता।
वैसे ही अनाकृत मन स्वतः ...
अपने आप को कोई सांचा। आकृति मत दो। सब सांचा एक तरह का कवच है। सब सांचे एक तरह की सुरक्षा हैं। सब सांचे एक प्रकार के आकृतिकरण ही है। खुले रहो, सांचों में मत ढलो।
वैसे ही अनाकृत मन स्वतः ...
यदि तुम आकृतियों में नहीं हो, यदि तुम बस खुले हो, तुम्हारे पास कोई कवच नहीं है, तुम तर्क से, संदेह से इससे-उससे अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे हो, तुम बस उपलब्ध हो...अनाकृत, असुरक्षित, खुले आकाश के नीचे, सब द्वार खुले होते है। फिर चाहे मित्र प्रवेश करे या शत्रु, कोई भी खुले रहने दो, परंतु सब द्वार खुले हैं। उस खुले पन में, तुम स्वयं में स्थित होते हो, तुम तथाता की अवस्था में होते हो, तुम रिक्त होते हो, तुम एक शून्य होते हो, और तुम जान लोगे कि सत्य क्या है:
पहचान जाते हैं रहस्यपूर्ण वृतों की गोलाई को ...
और तब तुम देखोगे कि इस तथाता से दो वृत उत्पन्न हो रहे हैं: एक है निर्वाण का, दूसरा है संसार का। तथाता के इस समुद्र में दो तरह कि लहरे उठ रही है: एक है पदार्थ की, दूसरी है मन की--परंतु दोनों लहरें हैं। और तुम दोनों के पार हो। अब न कोई विभाजन रहा और न ही कोई अंतर। सत्य न मन है, न पदार्थ, सत्य न संसार है, न निर्वाण, सत्य न पवित्र है न अपवित्र--सारे अंतर विलीन हो गए होते है।
यदि तुम परम सचाई में अपना मन लेकर आओ, यह तुम्हें परम सचाई को न देखने देगा। यह अपने-अपने असत्यों में से कुछ अपने साथ ले आएगा।
मैं एक घटना पढ़ रहा था। इस पर जरा ध्यान करो--
एक व्यक्ति मर कर स्वर्ग के मोती-जड़े द्वार के पास आया, द्वारपाल के पूछे जाने पर उसने अपना नाम बताया, ‘चार्ली झपट्टा वाला।’
‘मैं नहीं समझता कि तुम्हारे यहां आने की हमें कोई खबर है ’, उसे सूचित किया गया। ‘पृथ्वी के जीवन में तुम्हारा व्यवसाय क्या था?’
‘कबाड़ीवाला,’ आगंतुक ने कहा।
‘अच्छा,’ देवदूत ने कहा, ‘मैं अंदर जाऊंगा और पूछताछ करके आपको बाताऊंगा।’
जब वह वापस लौटा, चार्ली झपट्टावाल गायब हो चुका था--और साथ ही मोती-जड़े द्वार भी।
चार्ली झपट्टावाला-कबाड़ीवाला...तुम अपनी आदतें एकदम अंत तक ले जाते हो।
शायद जहां तक मनुष्य-निर्मित संसार का संबंध है, मन उपयोगी है। शायद जहां तक पदार्थ के संबंध में विचार का संबंध है, मन उपयोगी है। पर इस मन को तुम्हारी सच्चाई के अंतर्तम केंद्र तक ले जाना खतरनाक है। वहां यह बाधा है।
मुझे यह बात इस तरह से कहने दो: विज्ञान के जगत में तो संदेह उपयोगी है--सच तो यह है कि बिना संदेह के विज्ञान निर्मित ही नहीं होता। संदेह तो विज्ञान की विधि है, क्योंकि विज्ञान इतना प्रभावी हो गया है, अतीत में इतना सफल रहा है, ऐसा जान पड़ता है कि विज्ञान जिज्ञासा की एकमात्र विधि हो गया है। इसलिए जब तुम भीतर जाते हो, तब भी तुम संदेह के साथ ही जाते हो। यह एकदम से सही नहीं है। जब तुम बाहर जा रहे होते हो, तब संदेह तुम्हारे लिए सहायक है, तुम्हारे मार्ग का मार्ग-दर्शक बन जाता है, परंतु अगर तुम भीतर जाना चाहते हो, संदेह कम और कम और कम करते जाओ, और एक क्षण ऐसा भी आने दो जब संदेह बचे ही नहीं। अ-संदेह की उस दशा में, तुम केंद्र पर होगे। यदि तुम भीतर के जगत को जानना चाहते हो, श्रद्धा वहां उपयोगी साबित होगी।
अतीत में पूरब में यही तो घटना घटी है। हमने श्रद्धा के द्वारा आंतरिक सच्चाई को जाना, इसलिए हमने सोचा कि श्रद्धा के साथ हम विज्ञान को भी निर्मित कर सकते है। पूरब में हम किसी महान विज्ञान का निर्माण न कर सके--कुछ ऐसा जिसकी चर्चा की जा सके--कुछ खास नहीं। क्योंकि हमने श्रद्धा द्वारा भीतर प्रवेश किया हमने सोचा कि श्रद्धा ही जिज्ञासा की एकमात्र विधि है--यह बात भ्रम थी। हमने बाहर की वस्तुगत चीजों पर भी श्रद्धा का प्रयास किया और हम असफल हुए। जहां तक विज्ञान का संबंध है, पूरब असफल रहा है। पश्चिम संदेह द्वारा विज्ञान में सफल हुआ है, अब वही भ्रम वहां भी है, वे सोचते हैं कि संदेह ही जानने का एकमात्र सही और युक्तिसंगत उपाय है। परंतु ऐसा कदापि नहीं है। अब अगर तुम संदेह का उपयोग आंतरिक जगत में करो, तुम इतने ही सुनिश्चित ढंग से असफल होओगे जितना कि पूरब वैज्ञानिक विकास में असफल हुआ है।
वस्तुओं के विषय में संदेह अच्छा है, आत्म चेतनता के विषय में श्रद्धा अच्छी है। संदेह अच्छा है यदि तुम अपने केंद्र से परे हट रहे हो, परिधि की और श्रद्धा अच्छी है यदि तुम परिधि से दूर हट रहे हो अपने केंद्र की ओर। श्रद्धा और संदेह दो पंखों की भांति हैं।
भविष्य में जो मानवता पैदा होने वाली है, वह संदेह और श्रद्धा दोनों एक साथ करने में सक्ष्म होगी। वह सर्वोत्तम संश्लेषण होगा: पूरब और पश्चिम का संश्लेषण, विज्ञान और धर्म का संश्लेषण। जब एक व्यक्ति संदेह और श्रद्धा दोनों करने में समर्थ होता है--जब संदेह की आवश्यकता होती है, जब वह बाहर जा रहा होता है, वह संदेह करता है, और जब श्रद्धा की आवश्यता होती है, वह संदेह को अलग उठा कर रख देता है। और वह उस समय पूर्ण श्रद्धा से उसमें डूब जाता है, उस में उतर जाता है। और जो व्यक्ति दोनों में ही समर्थ है, वह दोनों के पार हो जाते है। निश्चय ही दोनों के पार, क्योंकि वह दोनों का उपयोग करेगा और वह जानेगा कि ‘मैं दोनों से अलग हूं।’ यही अनुभवातितता है, यह पार हो जाना महान स्वतंत्रता है। ठीक यही तो निर्वाण है: महान स्वतंत्रता।
इन सूत्रों पर ध्यान लगाओ। सरहा सरल शब्दों में महान बातें कह रहे हैं। वह अपनी महान अंतदृष्टि राजा पर बरसा रहा था। तुम भी इस महान अंतदृष्टि में सहभागी हो सकते हो। सराह के साथ तुम मानवीय सचाई में बहुत गहराई तक जा सकते हो।
और सदा स्मरण रखना: परम सच्चाई तक जाने का यही एक मात्र मार्ग है, क्योंकि वही तो तुम हो। कोई भी वही से तो चल सकता है जहां कि वह है। काम तुम्हारी वास्तविकता है, समाधिस्थ इसके द्वारा हो सकते हो। जीवन के उस परम तक पहुंच सकते हो, सच उसी पूर्ण समाधान का नाम समाधि है, जहां अब कोई संशय नहीं बचा सब शंका निवारण हो गई। पहुंच गए अपने घर, लौट आए तुम अपनी पूर्णता में, विलय हो गई बूंद सागर में। देह तुम्हारी वास्तविकता है, देहातितता इसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। बाहरीपन तुम्हारी वास्तविकता है। भीतरता इसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। बस जरा सा परिवर्तन तुम्हारी आंखें जो अभी बाहर की और ही देख रही है, उन्हें अंदर की तरफ मोड़ना ही तो है। और उन्हें भीतर की और मोड़ा जा सकता है।
आज इतना ही

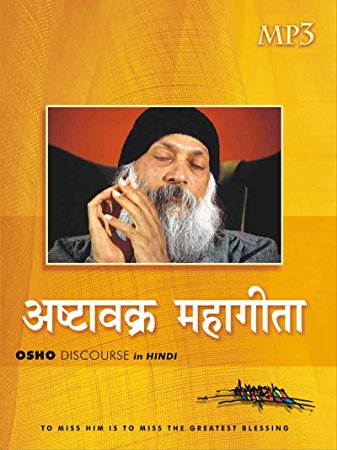

Comments
Post a Comment