बंधन क्या? मोक्ष क्या? विद्या और अविद्या क्या? जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय--ये चार अवस्थाएं क्या हैं?अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये पांच कोश क्या हैं? कर्ता, जीव, पंचवर्ग, क्षेत्रज्ञ, साक्षी, कूटस्थ और अंतर्यामी का अर्थ क्या है? इसी प्रकार जीवात्मा, परमात्मा और माया--ये तत्व क्या हैं? परमात्मा से प्रार्थना के बाद जिज्ञासा का प्रारंभ है।
प्रार्थना के बाद ही जिज्ञासा हो सकती है। प्रार्थना हृदय को उस स्थिति में ला देती है, उस ग्राहक और संवेदनशील मनोदशा को पैदा कर देती है, जहां जिज्ञासा मात्र कुतूहल नहीं रह जाती, मुमुक्षा बन जाती है। प्रार्थना से रहित जो जिज्ञासा है, वह केवल बौद्धिक खिलवाड़ है। और जिसने प्रार्थना नहीं की और पूछा है, उसने पूछा ही नहीं। जिसके घर का द्वार बंद है, अंधेरे में बैठ कर जो पूछ रहा है, सूर्य क्या है, प्रकाश क्या है, वह पूछता रहे, उत्तर उसे नहीं मिल पाएगा।
और आदमी के मन का बड़े से बड़ा खेल यह है कि जब उत्तर नहीं मिलता तो आदमी खुद अपने उत्तर बना लेता है--अंधेरे में ही, बिना सूर्य को जाने ही--या तो कहने लगता है कि सूर्य नहीं है...इसलिए नहीं कि उसने जान लिया कि सूर्य नहीं है, इसीलिए कि चूंकि वह नहीं जान पाया, और जिसे वह नहीं जान पाया उचित है कि वह उसे इनकार कर दे; क्योंकि जिसे हम नहीं जान पाते, अगर हम उसे इनकार न कर पाएं तो मन में एक बेचैनी खड़ी ही रह जाती है। इनकार करते से बेचैनी भी खो जाती है; हम अपने अंधेरे में ही आश्वस्त हो जाते हैं। लेकिन जिसने घर के द्वार नहीं खोले वह कितना ही पूछे कि सूर्य क्या है, प्रकाश क्या है, उत्तर उसे नहीं मिल सकता। नहीं मिले उत्तर, तो वह यह भी कर सकता है कि इनकार भी न करे, अपने ही मन का सूर्य गढ़ ले, और कहने लगे सूर्य है--और अपनी ही मनोरचना कर ले, अपने ही सिद्धांत निर्मित कर ले। वे सिद्धांत उतने ही झूठे हैं, जितना इनकार करना झूठा है।
अंधेरे में खड़ा नास्तिक भी उतना ही झूठा है, जितना अंधेरे में खड़ा आस्तिक झूठा है। नहीं जिसने जाना, उसका यह कहना भी व्यर्थ है कि ईश्वर नहीं है, उसका यह कहना भी व्यर्थ है कि ईश्वर है; ये दोनों बातें ही व्यर्थ हैं। और बड़ा मजा है कि अंधेरे में बड़ी कलह और बड़ा विवाद चलता है उनके बीच, जिन दोनों को ही पता नहीं है।
अज्ञात बहुत विवादग्रस्त है। अज्ञान जानता नहीं, लेकिन मुखर बहुत है। विवाद तो किया ही जा सकता है, मतवाद तो खड़े किए ही जा सकते हैं। वस्तुतः अंधेरे में ही मतवाद खड़े होते हैं; प्रकाश में कोई वाद नहीं है। प्रकाश काफी है, वाद की कोई जरूरत नहीं। सब सिद्धांत अंधेरे में निर्मित होते हैं, प्रकाश में सिद्धांतों की कोई भी जरूरत नहीं है। जहां सत्य प्रकट है वहां शब्द खो जाते हैं; और जहां सत्य ही समक्ष है वहां सिद्धांत को बनाने का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। सिद्धांत सब्स्टीट्यूट है, परिपूरक है; सत्य का पता नहीं है तो सिद्धांत बना कर हम सत्य की जगह उसे खड़ा कर लेते हैं।
ठीक जिज्ञासा प्रार्थना से शुरू होती है। जब मैं ऐसा कहता हूं, तो उसका अर्थ यह है कि जो सूर्य को जानने चला है, कम से कम एक शर्त पूरी कर दे कि अपने मकान के द्वार खोल दे; सूर्य को जानने की आकांक्षा जगी है तो कम से कम अपने द्वार-दरवाजे तो खोल ले, ताकि सूर्य उत्तर देना चाहे तो उत्तर दे सके।
सूर्य की शक्ति विराट है, लेकिन फिर भी आपका द्वार तोड़ कर भीतर प्रवेश नहीं करेगी; आपके दरवाजे पर थपकी भी सूरज नहीं देगा। इस जगत में सत्य किसी के जीवन में ट्रेसपास नहीं करता, किसी के जीवन का अतिक्रमण नहीं करता; सत्य किसी के जीवन में किसी भी भांति की गुलामी नहीं लाता, बंधन नहीं लाता, इसलिए सत्य मुक्ति है। सत्य जबर्दस्ती आरोपित नहीं होता। जब तक आप ही तैयार न हों, सत्य आपके द्वार पर खड़ा रहेगा, लेकिन थपकी भी नहीं देगा, द्वार को खटखटाएगा भी नहीं। आपकी तैयारी, आपका हृदय से दिया गया निमंत्रण ही उसका आगमन बन सकता है। लेकिन आपके निमंत्रण का क्या अर्थ है, जब तक आपका द्वार खुला न हो! जिस अतिथि को आप पुकारते हैं, उसके लिए द्वार पर बैठ कर प्रतीक्षा भी तो करनी चाहिए। इसलिए प्रार्थना से प्रांरभ है। प्रार्थना है हृदय के द्वार को खोलने की विधि।
अगर प्रार्थना से रहित जिज्ञासा है, तो वह जिज्ञासा खोज की कम, संदेह की ज्यादा होती है। वह इसलिए नहीं होती है कि हम खोजने निकले हैं, वह इसलिए होती है कि हम संदेह करने निकले हैं। और जो संदेह करने ही निकला है, उसका संदेह रुग्ण हो जाता है, बीमार हो जाता है। लेकिन जो प्रार्थनापूर्ण हृदय से खोलता है द्वार, ऐसा नहीं कि उसे संदेह करने का हक नहीं रह जाता, सच तो यह है कि उसे ही संदेह करने का हक मिलता है; क्योंकि अब संदेह केवल समाधान की आकांक्षा का हिस्सा है; अब संदेह विनाशक नहीं है, सृजनात्मक है। अब संदेह इसीलिए है कि मार्ग के सब कंटक कैसे दूर हो जाएं; अब प्रश्न इसीलिए है कि उत्तर कैसे निकट आ जाए। अब प्रश्न किसी बीमार चित्त की भाग-दौड़ नहीं, अब संदेह किसी रुग्ण-चित्त का रोग नहीं, अब एक स्वस्थ व्यक्ति की खोज है। ‘श्रद्धापूर्ण संदेह’ शब्द बहुत उलटा दिखाई पड़ेगा। लेकिन हम एक तरफ से समझें तो खयाल में आ जाएगा; संदेहपूर्ण श्रद्धा से समझें तो खयाल में आ जाएगा। हम श्रद्धा भी करते हैं, तो वह संदेहपूर्ण होती है। हम किसी पर श्रद्धा भी करते हैं, तो वह संदेहपूर्ण होती है; उसमें संदेह होता ही है। असल में हम श्रद्धा ही इसलिए करते हैं कि भीतर संदेह होता है, उसे दबाने के लिए श्रद्धा कर लेते हैं। और भीतर संदेह हो और ऊपर श्रद्धा हो, तो श्रद्धा कमजोर होती है; क्योंकि जो भीतर है वही शक्तिशाली है; जो ऊपर है वह कमजोर होगा--जो परिधि पर है वह कमजोर होगा, जो केंद्र में है भीतर हृदय के वही शक्तिशाली है।
तो भीतर तो संदेह होता है, श्रद्धा ऊपर से थोप लेते हैं वस्त्रों की भांति। जैसे वस्त्र आपकी नग्नता को नहीं मिटाते, केवल छिपाते हैं, ऐसे ही वस्त्रों की भांति थोपी गई श्रद्धा भी संदेह को मिटाती नहीं, सिर्फ छिपाती है। इससे उलटा भी होता है, जिसको मैं कह रहा हूं, श्रद्धापूर्ण संदेह। श्रद्धा तो होती है हृदय के केंद्र पर, परिधि पर संदेह होता है। वह संदेह श्रद्धा को और प्रगाढ़ करने की यात्रा का हिस्सा है; क्योंकि जिसने संदेह ही नहीं किया वह श्रद्धा कैसे कर सकेगा? लेकिन है वह अति श्रद्धापूर्ण।
बुद्ध से मौलुंकपुत्त ने कहा है, उनके एक शिष्य ने, पूछता हूं आपसे, इसलिए नहीं कि आप पर संदेह है, इसलिए कि अपने पर संदेह है; पूछता हूं आपसे, इसलिए नहीं कि आप जो कहते हैं उस पर संदेह है, बल्कि इसलिए कि आप जो कहते हैं उसे मैं समझ पाता हूं, इस पर संदेह है; पूछता हूं आपसे, इसलिए नहीं कि आप जहां पहुंच गए हैं उस पर मुझे संदेह है, पूछता हूं सिर्फ इसीलिए कि इतनी दूर की यात्रा, इतना विराट स्वप्न, मुझे अपने पैरों पर संदेह है; पूछता हूं इसलिए कि मेरा भरोसा बढ़े; पूछता हूं इसलिए कि मेरी श्रद्धा प्रगाढ़ हो। प्रार्थना से जब भी कोई पूछता है, तो उसके हृदय के द्वार होते हैं खुले; संदेह लेकर वह नहीं आता, सिर्फ प्रश्न लेकर आता है। प्रश्नों के उत्तर हो सकते हैं, संदेहों के उत्तर नहीं हो सकते; क्योंकि जिसे संदेह ही करने हैं वह आपके हर उत्तर का संदेह किए चला जाता है।
संदेह जो है वह इनफिनिट रिग्रेस है। आप एक उत्तर देते हैं, उस पर उसे संदेह है; आप दूसरा देते हैं, उस पर उसे संदेह है; संदेह उसकी भूमिका है। तो आप जो भी कहते हैं, उस पर उसे संदेह है। तब तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन संदेह अगर केवल खोज का हिस्सा है, जस्ट ए मेथडोलॉजी, एक विधि, अंत नहीं, लक्ष्य नहीं, साध्य नहीं; संदेह अगर भूमिका नहीं है, भूमिका जिज्ञासा है, तो संदेह बड़ा सहयोगी है।
तो श्रद्धापूर्ण संदेह।...प्रार्थनापूर्ण जिज्ञासा।
पहला ही प्रश्न पूछता है--पहला ही प्रश्न पूछा गया है सर्वसार में: ‘‘बंधन क्या?’’
खयाल करें! हम भी पूछते हैं तो पूछते हैं: ईश्वर क्या?...ईश्वर है या नहीं? मोक्ष क्या?...मुक्ति है या नहीं? आत्माक्या?...आत्मा है या नहीं?
हम वहां से शुरू करते हैं जहां अंत होना चाहिए। बीमार आदमी पूछता है: स्वास्थ्य क्या? लेकिन समझदार सदा पूछेगा...बीमार है तो...कि बीमारी क्या है? निदान तो बीमारी से शुरू होगा। इसलिए सर्वसार पहला प्रश्न उठाता है: ‘बंधन क्या?’
वही है रोग, वही है बीमारी; बंधे हैं हम। कारागृह में पड़ा है कोई--जंजीरों से कसा, बेड़ियों में बंधा, वह पूछता है: स्वतंत्रता क्या? उसने कभी स्वतंत्रता जानी नहीं, समझें कि सदा से बंधा है, जन्म से ही बंधा है--जब से उसने जाना है अपने को तब से बंधा है; उसका जानना और बंधन दोनों साथ-साथ जुड़े हैं; पूछता है, स्वतंत्रता क्या? समझ में शायद उसे न आ पाए। ठीक सवाल उसने उठाया नहीं। जो वह समझ सकता है, अभी उसे वही पूछना चाहिए।
बुद्धिमान खोजी वह है, जो उस सवाल को पूछता है, जिसके जवाब को अभी वह, अभी समझा सकेगा। और शायद उसे समझ ले तो दूसरी बात भी समझ में आ जाए।
इसलिए पहला सवाल है: बंधन क्या? कहां मैं बंधा हूं? क्योंकि जो आदमी सदा से बंधा है उसे यह भी पता नहीं होता कि बंधन क्या है! बंधन को पहचानने के लिए भी स्वतंत्र होने का कोई अनुभव चाहिए। आपके हाथों में जंजीरें डाल दी जाएं, आप पहचान जाएंगे कि जंजीरें डाल दी गईं। लेकिन अगर एक बच्चा पैदाइश के साथ जंजीरों को लेकर पैदा हो, तो क्या कभी पहचान पाएगा कि ये जंजीरें हैं? वह उसके शरीर का हिस्सा होगा। और अगर आप उसकी जंजीरें तोड़ने लगें तो वह चीखेगा, चिल्लाएगा कि मुझे मिटाना चाहते हो! ये जंजीरें उसका प्राण हैं; ये जंजीरें अलग नहीं हैं, ये जंजीरें उसका होना हैं।
और हम ऐसे ही हैं। जब से हम हैं, जब से हमने जाना है कि हम हैं, हमारे होने का बोध और हमारा कारागृह एक साथ हैं। हमें स्वतंत्रता का कोई अनुभव ही नहीं; हमने कभी आकाश में उड़ कर देखा ही नहीं; हमारे पंख कभी खुले आकाश में खुले नहीं; हमने उन्हें सदा बंद ही जाना है। हमारे पंख उड़ने के काम में भी आ सकते हैं, इसका भी हमें कोई पता नहीं। हम कारागृह में ही पैदा हुए और बड़े हुए हैं; कारगृह ही हमारा जीवन है।
तो जो सम्यक जिज्ञासा है, वह शुरू होगी कि बंधन क्या? अभी तो हमें यह भी पता नहीं कि गुलामी क्या है? इतने गहरे हैं हम गुलामी में--गुलामी ही हैं हम--कैसे पहचानें कि गुलामी क्या है? एक व्यक्ति पैदा हुआ है और उसके सिर में दर्द रहा है जीवन भर, तो सिरदर्द ओर सिर में वह फर्क नहीं कर सकता; उसने सिर को सदा दर्द के साथ ही जाना है।
पश्चिम की एक बहुत विचारशील महिला सिमोन वेल ने लिखा है कि तीस साल की उम्र तक उसे पता ही नहीं था कि सिरदर्द क्या है? इसलिए नहीं कि उसे कभी सिरदर्द नहीं हुआ, इसलिए कि उसे सदा ही सिरदर्द रहा; उसने कभी जाना ही नहीं कि सिर भी बिना दर्द के हाता है। तो दर्द और सिर में कोई फर्क नहीं हो सका। तीस साल की उम्र में जब पहली दफा उसका सिरदर्द ठीक हुआ, तब उसे पता चला कि वह सिरदर्द था, सिर नहीं था।
जिसके साथ हम बड़े होते हैं, उसे हम अलग नहीं जान पाते। इसीलिए तो हम शरीर को भी अलग नहीं जान पाते, क्योंकि हम उसी के साथ बड़े होते हैं। इसलिए तादात्म्य हो जाता है, आइडेंटिटी हो जाती है; उसी के साथ एक हो जाते हैं। इसलिए हम मन के साथ अपने को पृथक नहीं जान पाते, क्योंकि हम उसी के साथ बड़े होते हैं, तादात्म्य हो जाता है।
ऋषि पहला सवाल इस उपनिषद में उठा रहा है, वह यह कि ‘बंधन क्या है?’
ऐसा समझें: कि ऋषि से पूछा जा रहा है, शिष्य पूछ रहा है कि बंधन क्या है? यह उपनिषद एक बहुत गहरा डायलॉग है, एक संवाद है। बंधन समझ में आ जाए तो ही जो सदा से बंधा है उसे स्वतंत्रता के संबंध में कोई, कोई दर्शन, कोई स्वप्न, कोई आकार पैदा हो सकता है।
जो आदमी सदा बीमार रहा है उसके स्वास्थ्य की परिभाषा नकारात्मक ही हो सकती है। वह यही समझ सकता है कि स्वास्थ्य का अर्थ होगा जहां यह बीमारी नहीं है। जो आदमी कारामृह में रहा है, जंजीरों में रहा है, वह स्वतंत्रता की कोई पाजिटिव, विधायक परिभाषा नहीं समझ सकता। वह इतना ही समझ सकता है कि स्वतंत्रता का अर्थ है जहां ये जंजीरें नहीं होंगी; जहां ये कारागृह की दीवालें नहीं होंगी, जहां मुझे रोकने वाला द्वार पर कोई संगीन लिए पहरेदार नहीं होगा; जहां मैं जहां जाना चाहूं, जो करना चाहूं, कर सकूंगा। यह नकारात्मक परिभाषा ही उसकी समझ में आ सकती है। लेकिन इस परिभाषा के पहले जेलों की दीवाल को, कारागृह को, द्वार पर खड़े संतरी की व्यवस्था को, हाथ में पड़ी जंजीरों को ठीक से समझ लेना जरूरी है।
कॉकेसस का एक बहुत अदभुत फकीर गुरजिएफ कहा करता था कि मैंने सुना है एक जादूगर के संबंध में कि उसने बहुत सी भेड़ें पाल रखी थीं। और रोज एक भेड़ को वह काटता और अपना भोजन तैयार करवाता। सैकड़ों भेड़ें यह देखती रहतीं, लेकिन फिर भी भेड़ों को याद न आती यह बात कि आज नहीं कल हम भी काटे जाने को हैं। उस जादूगर के पास एक मेहमान ठहरा हुआ था, उस मेहमान ने कहा कि ये भेड़ें बड़ी अदभुत मालूम होती हैं। इनके सामने ही तुम रोज भेड़ों को काटते रहते हो, फिर भी ये भेड़ें मस्त घूमती रहती हैं; इन्हें खयाल नहीं आता क्या कि हम भी कल काटे जाने को हैं? किसी भी दिन यह छुरी हमारी गर्दन पर भी पड़ेगी?
उस जादूगर ने कहा कि मैंने इन भेड़ों को बेहोश करके सभी को एक सुझाव दे रखा है, और वह यह: प्रत्येक के कान में मैंने उसकी बेहोशी में कह दिया है कि तुम भेड़ नहीं हो, बाकी सब हैं--तुम भेड़ नहीं हो, बाकी सब भेड़ें हैं; सब कटेंगी, तुम भर नहीं कटोगी। इसलिए ये निश्चिंत हैं; और ये किसी को कटते देख कर भागती नहीं हैं।
उस मेहमान ने पूछा: और भी हैरानी की बात है कि तुम इन्हें कभी बांधते नहीं! ये कभी भटक नहीं जातीं, खो नहीं जातीं?
उसने कहा: मैंने इन्हें यह भी कह रखा है कि तुम परम स्वतंत्र हो, तुम बंधी हुई नहीं हो; क्योंकि बंधन से तो कोई भागता है, जब कोई स्वतंत्र ही हो तो भागने का कोई सवाल ही नहीं। बंधन हो तो भागने का खयाल भी पैदा होता है--भाग जाओ, लेकिन बंधन हो ही न, परम स्वतंत्र हो, भागने की जरूरत ही नहीं।
गुरजिएफ कहा करता था कि आदमी करीब-करीब ऐसी ही स्थिति में है; वह अपने कारागृह को अपना महल मानता है। तो उससे छूटने का सवाल ही नहीं है, बल्कि कोई छुड़ाने आ जाए तो वह सुरक्षा का इंतजाम करेगा कि तुम हमारे दुश्मन हो, महल से छुड़ाना चाहते हो! आदमी अपनी जंजीरों को आभूषण मानता है; वह उसका श्रृंगार हैं। अगर उसके आभूषण छीनने जाओगे तो वह तलवार निकाल कर खड़ा ही हो जाएगा।
तो हम जीसस को ऐसे ही थोड़े ही सूली पर लटका देते हैं! और सुकरात को हम ऐसे ही बेकार थोड़े ही जहर पिला देते हैं! इसीलिए कि हमारे आभूषण ये लोग छीनने की कोशिश करते हैं; ये हमारे दुश्मन हैं। जिसे वे हमारी जंजीरें कहते हैं, वे हमारे श्रृंगार हैं। और जिसे वे कहते हैं, तुम्हारा कारागृह, वह हमारा राजभवन है; और जिसे वे कहते हैं, तुम्हारी गुलामी, वह हमारा जीवन है; जिसे वे कहते हैं, दुख, उनमें ही हमारा सारा सुख छिपा है।
इसलिए पहली बात, गुरजिएफ कहता था, जान लेनी जरूरी है--अगर किसी कैदी को मुक्त होना हो, तो पहली बात जाननी जरूरी है कि वह कैदी है; बाकी नंबर दो की बातें हैं। किसी गुलाम को मुक्त होना हो, तो उसे पहली बात जाननी जरूरी है कि वह गुलाम है। यह उसकी चेतना में इतनी गहराई से घुस जानी चाहिए, प्रवेश कर जानी चाहिए कि उसके प्राण पीड़ित हो उठें और मुक्त होने की आकांक्षा से भर जाएं।
क्या है बंधन? दूसरा प्रश्न...ठीक दूसरा तब उठ सकता है: ‘‘क्या है मोक्ष?’’
‘‘कथं बंधः--क्या है बंधन? कथं मोक्षः--क्या है मोक्ष?’’
बुद्ध के पास जाकर यदि आप पूछते कि क्या है मोक्ष, तो बुद्ध कभी उत्तर नहीं देते थे; अगर आप पूछते: क्या है बंधन, क्या है मोक्ष, तो उत्तर मिल सकता था; क्योंकि जिसने अभी ठीक सवाल ही नहीं पूछा उसे ठीक जवाब नहीं दिया जा सकता। गलत सवालों के ठीक जवाब नहीं होते। और आप क्या पूछते हैं, यह आपकी मनोदशा की खबर देते हैं। बंधन को समझ कर ही मोक्ष को समझा जा सकता है।
और तब प्रश्न है: ‘‘विद्या क्या, अविद्या क्या?’’
बंधन क्या, मोक्ष क्या? विद्या क्या? क्या है ज्ञान? ठीक होता कि जैसा पहला प्रश्न है: बंधन क्या, मोक्ष क्या; हमें लगेगा, पूछना था--अविद्या क्या, विद्या क्या? लेकिन वैसा नहीं पूछा है। और यह सांयोगिक नहीं है। पहले पूछना था, अज्ञान क्या, ज्ञान क्या? वैसा नहीं पूछा है; क्योंकि यहां विद्या से प्रयोजन ही दूसरा है। यहां विद्या से मतलब है...बंधन क्या, मोक्ष क्या? और जब पूछता है उपनिषद, विद्या क्या? तो उसका मतलब है: मुक्त होने का उपाय क्या? विद्या का मतलब ही यह होता है। विद्या का मतलब होता है: मुक्त होने का उपाय क्या? विद्या का अर्थ कभी भी यह नहीं होता जैसा हम समझते हैं।
मान लिया कि कारागृह में पड़े हैं, और मान लिया कि इस कारागृह के बाहर एक मुक्त गगन है, और गगन में उड़ा जा सकता है; और माना कि अंधेरे की दीवालों के पार एक सूर्य भी है, और उस सूर्य के साथ एक हुआ जा सकता है; और माना कि इस देह के पार अमृत का वास है--लेकिन मार्ग क्या? विधि क्या? यह भी पता चल जाए कि बंधन क्या है, और मोक्ष क्या है, और यह पता न हो कि द्वार कहां, मार्ग कहां--निकलेंगे कैसे, पहुंचेंगे कैसे--क्या करें? तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। बुद्ध ने चार आर्य सत्य कहे हैं, दि फोर फाउंडेशनल ट्रूथ्स, चार बुनियादी सत्य। और बुद्ध ने कहा है, चार को जो जान ले वह सबको जान लेता है। पहला कि आदमी दुख में है; पहला आर्य सत्य: दुख। दूसरा कि आदमी के दुख में होने के कारण हैं--अकारण दुख में नहीं है; क्योंकि अगर अकारण दुख में हो तो छुटकारे का कोई उपाय नहीं हो सकता। और तीसरा...क्योंकि कारण भी हो, आदमी दुख में भी हो, लेकिन अगर कोई मार्ग और विधि न हो, तो भी दुख के बाहर नहीं हो सकता। तो बुद्ध ने कहा: पहला सत्य, ‘दुख’, दूसरा सत्य, ‘दुख के कारण’; और तीसरा सत्य, ‘दुख-मुक्ति का उपाय।’ लेकिन दुख भी हो, दुख के कारण भी हों, दुख-मुक्ति का उपाय भी हो, लेकिन दुख-मुक्ति से छूटने की संभावना न हो...ऐसी कोई अवस्था ही न होती हो जहां आदमी दुख के बाहर हो जाए, तो हम एक दुख से छूट कर दूसरे दुख में पहुंच जाएंगे। तो बुद्ध ने चौथा आर्य सत्य कहा है: ‘दुख मुक्ति की अवस्था है।’ बुद्ध ने कहा: बस, ये चार काफी हैं। यहां विद्या से...जब पूछा जा रहा है, विद्या क्या? कैसे मुक्त हो जाएं? इसका मार्ग क्या, इसकी विधि क्या, इसका उपाय क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि बंधन हैं, कारागृह है, दुख है, और आदमी निरुपाय है--कोई उपाय नहीं! तो फिर संघर्ष व्यर्थ है; फिर हम जहां हैं वही संतुष्ट हो जाना उचित है; फिर जो है उसी को नियति मान लेना चाहिए--वही भाग्य है; उससे बाहर होने का कोई कारण नहीं है। इसलिए फिर कारागृह को महल मानना ही उचित है--जिसमें रहना ही हो, और जिसके बाहर जाना हो ही न सकता हो, फिर उसको कारागृह मान कर अकारण दुख पाना व्यर्थ है।

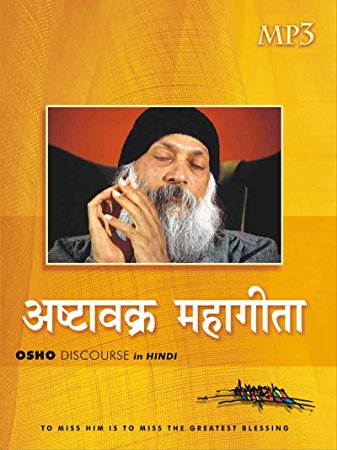

Comments
Post a Comment